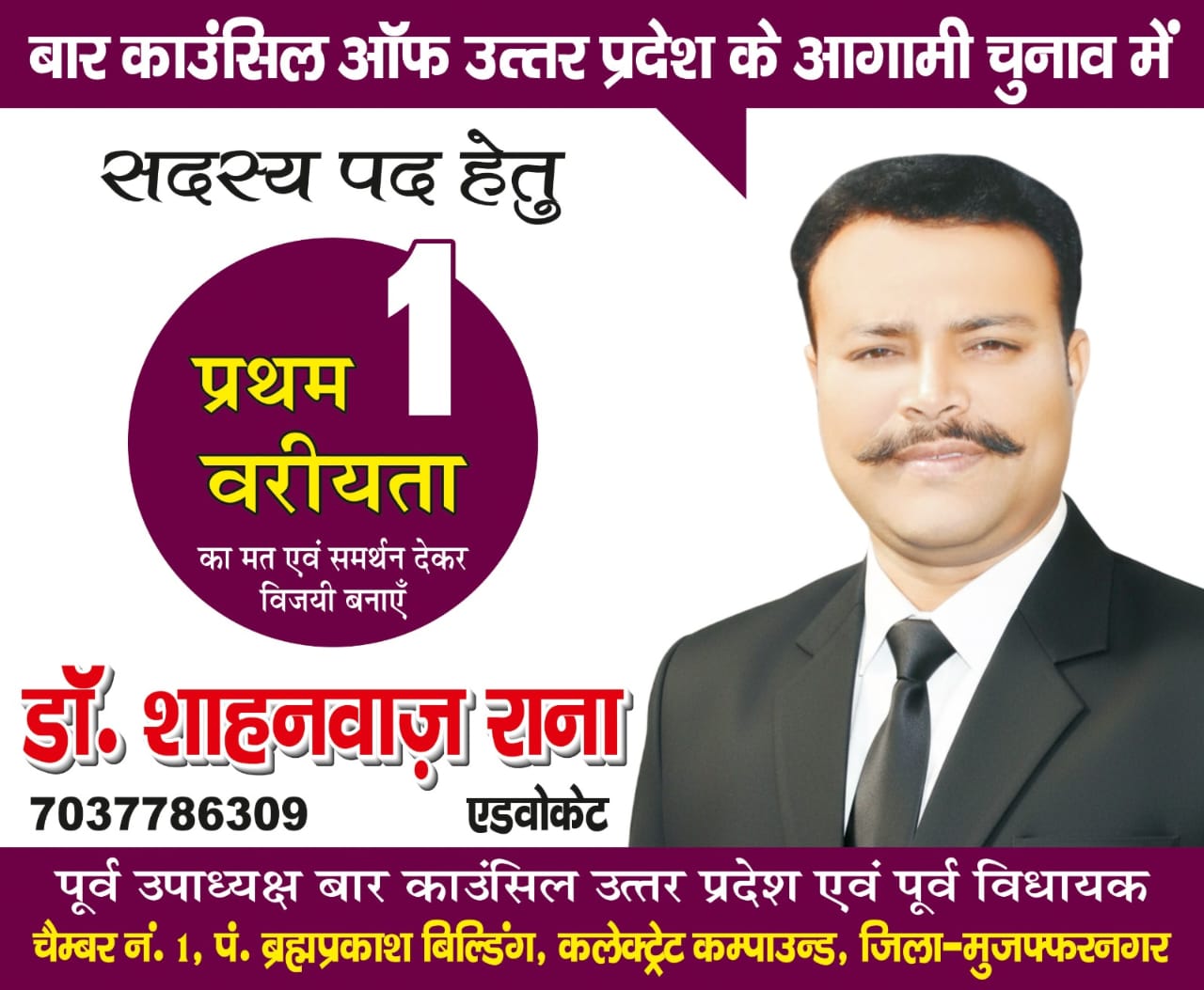Supreme Court to deliver interim verdict on constitutional validity of Waqf Amendment Act 2025.
वक्फ संपत्तियों का भविष्य तय करेगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश
संवैधानिक वैधता की परीक्षा: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025
भारत का लोकतंत्र अक्सर ऐसे मुकाम पर आकर ठहरता है जहाँ धार्मिक आस्था और संवैधानिक व्यवस्था आमने-सामने खड़ी दिखाई देती हैं। वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 इन्हीं पेचीदा बहसों का हिस्सा है। इस कानून ने पूरे मुल्क में गहरी हलचल मचा दी है। कोई इसे सुधार की दिशा मानता है, तो कोई इसे धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर हमला बताता है।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सोमवार को इस पर अपना अंतरिम फैसला सुनाने जा रही है। इस फैसले से यह साफ होगा कि क्या राज्य को धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप का अधिकार है, या यह समुदायों के दायरे में ही सीमित रहना चाहिए।
वक्फ की पृष्ठभूमि और सामाजिक भूमिका
वक्फ संस्था भारतीय उपमहाद्वीप की सदियों पुरानी परंपरा है। यह व्यवस्था न सिर्फ धार्मिक जरूरतों से जुड़ी बल्कि तालीमी इदारों, अस्पतालों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों और गरीबों की मदद जैसी कई सामाजिक जरूरतों को भी पूरा करती रही है।
इतिहास : मुगल दौर से लेकर ब्रिटिश राज तक वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल सामुदायिक भलाई में होता रहा।
सामाजिक महत्व : भारत में लाखों एकड़ जमीन और अरबों रुपये की संपत्तियाँ वक्फ बोर्डों के अधीन हैं।
चुनौतियाँ : भ्रष्टाचार, गलत प्रबंधन और राजनीतिक हस्तक्षेप लंबे समय से विवाद का विषय रहे हैं।
आज का शाह टाइम्स ई-पेपर डाउनलोड करें और पढ़ें
अधिनियम 2025 की प्रमुख विशेषताएँ
सरकार का कहना है कि इस अधिनियम से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं –
वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य डिजिटलीकरण और रिकॉर्ड पंजीकरण।
केंद्र और राज्य स्तर पर वक्फ बोर्डों की निगरानी प्रक्रिया।
वित्तीय लेन-देन पर सख्त ऑडिट व्यवस्था।
विवादों के निपटारे के लिए विशेष ट्रिब्यूनल का गठन।
गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति पर रोक का आश्वासन, जिससे धार्मिक भावनाओं की हिफाजत बनी रहे।
केंद्र सरकार का पक्ष
केंद्र ने अदालत में स्पष्ट कहा कि वक्फ संपत्तियों का कई जगह गलत इस्तेमाल हुआ है।
दुकानों और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जमीन का दुरुपयोग।
ऐतिहासिक स्मारकों में अवैध निर्माण।
आय का सही हिसाब न देना।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि संसद द्वारा पारित किसी कानून को रोकना तभी संभव है जब उसकी असंवैधानिकता बिल्कुल स्पष्ट हो। उन्होंने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक आस्था पर चोट पहुँचाना नहीं बल्कि प्रशासन को पारदर्शी बनाना है।
याचिकाकर्ताओं की दलीलें
दूसरी ओर 100 से अधिक याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गईं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि –
यह अधिनियम अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।
वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी।
सरकार धार्मिक संपत्तियों को नियंत्रित कर अपनी राजनीतिक मंशा पूरी करना चाहती है।
अल्पसंख्यक अधिकारों पर सीधा हमला है, जिससे भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि पर सवाल उठेंगे।
विश्लेषण : धर्म और कानून की जटिल जंग
यह मुद्दा केवल कानूनी दलीलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक और राजनीतिक आयाम भी हैं।
कानूनी दृष्टिकोण
अनुच्छेद 25 : सभी नागरिकों को धार्मिक आस्था और पूजा का अधिकार।
अनुच्छेद 26 : धार्मिक संस्थाओं को अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार।
सवाल यह है कि क्या राज्य की निगरानी धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करती है या यह “सार्वजनिक व्यवस्था” की श्रेणी में उचित ठहराई जा सकती है।
सामाजिक दृष्टिकोण
वक्फ संस्थाएँ गरीबों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का बड़ा साधन हैं। अगर उन पर अत्यधिक नौकरशाही नियंत्रण हुआ तो इन सेवाओं पर असर पड़ सकता है।
राजनीतिक दृष्टिकोण
विपक्ष इसे “अल्पसंख्यकों को कमजोर करने की साजिश” बताता है, जबकि सरकार इसे “सुधार और पारदर्शिता का प्रयास” कहती है।
प्रतिपक्षी नजर
यह तर्क भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वक्फ बोर्डों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। कई रिपोर्टों में करोड़ों रुपये की हेराफेरी उजागर हुई है।
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अधिनियम सही ढंग से लागू हुआ तो वक्फ संपत्तियाँ गरीब तबके के लिए और भी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। यानी निगरानी को पूरी तरह नकारना भी उचित नहीं होगा।
वैश्विक परिप्रेक्ष्य
दुनिया के कई मुल्कों में धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन राज्य की निगरानी में होता है।
तुर्की : यहाँ वक्फ संपत्तियों पर सख्त सरकारी निगरानी है।
मिस्र : धार्मिक संपत्तियों का केंद्रीकृत प्रबंधन होता है।
पाकिस्तान : वहाँ भी वक्फ बोर्ड सरकारी अधीनस्थ हैं।
भारत के मॉडल में संतुलन ढूँढना सबसे बड़ी चुनौती है – धार्मिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक पारदर्शिता के बीच।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल एक अधिनियम की संवैधानिकता तय नहीं करेगा बल्कि आने वाले वर्षों के लिए धर्म और राज्य के रिश्तों की नई परिभाषा भी तय करेगा।
क्या अदालत धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता को प्राथमिकता देगी या राज्य की पारदर्शिता की दलील को मान्यता देगी? यह फैसला भारत के लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।