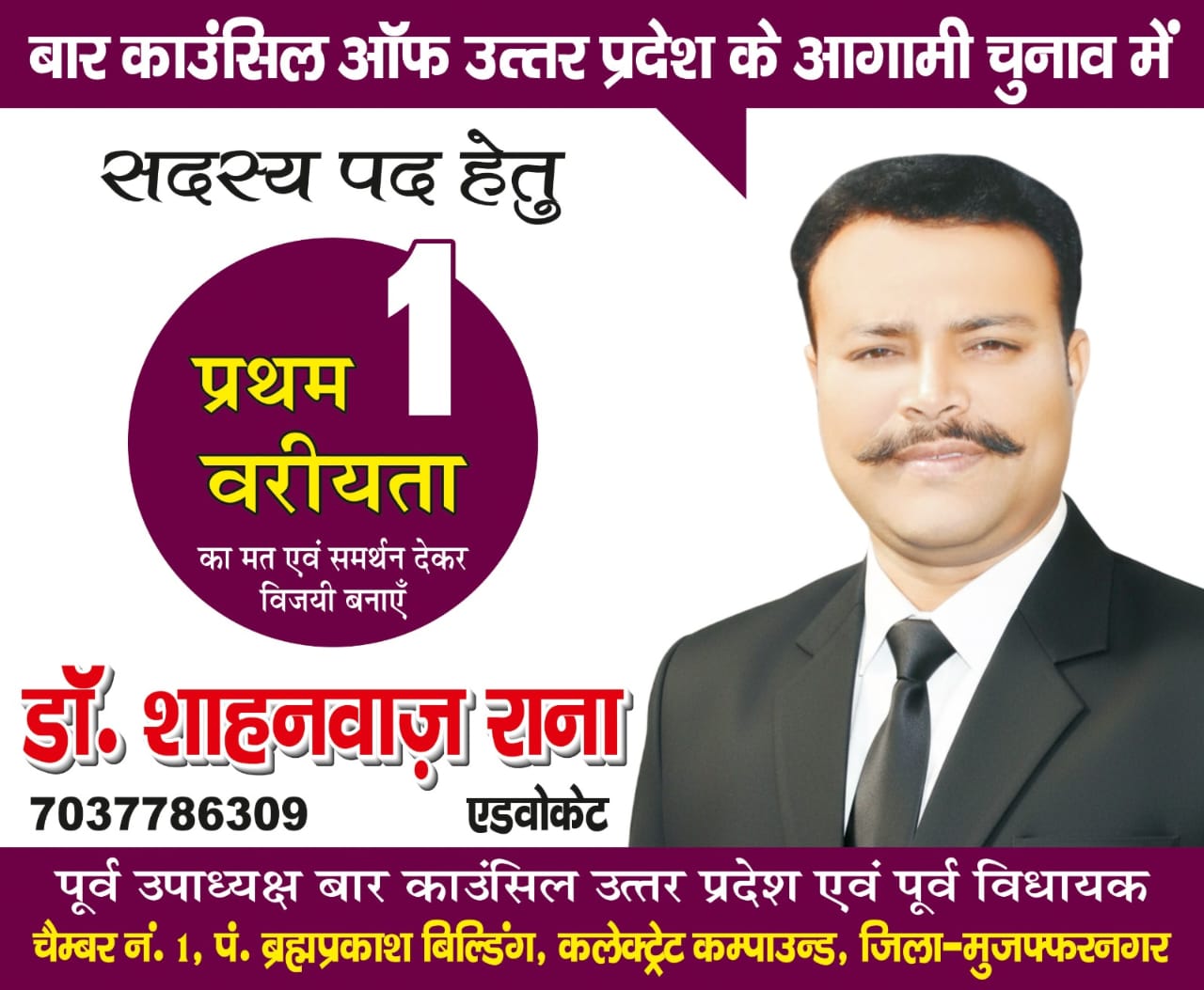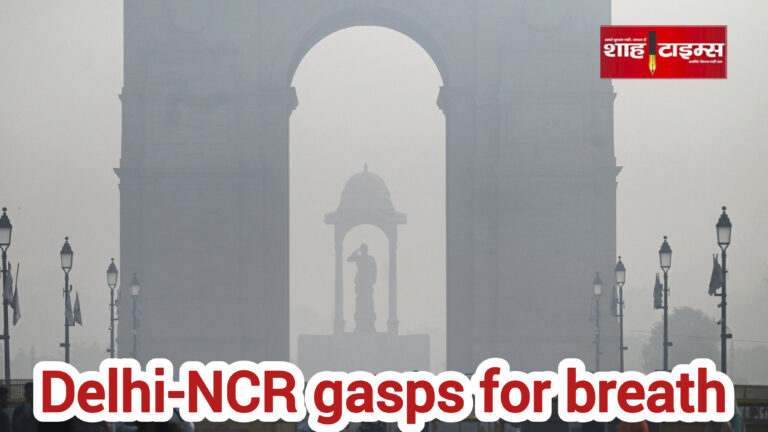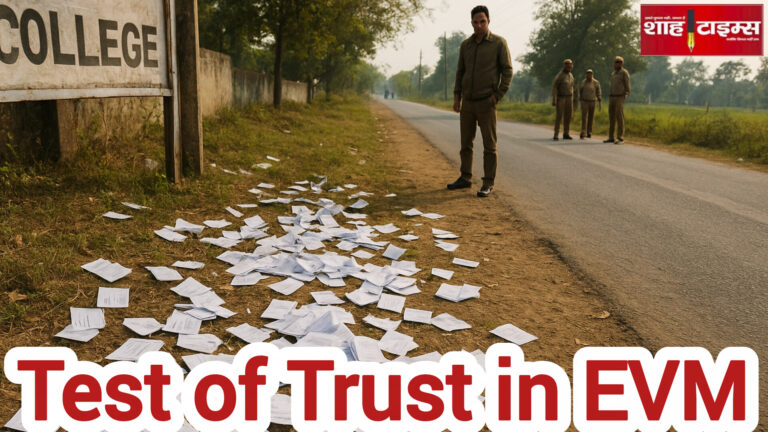UP caste order controversy between Yogi Adityanath govt and Akhilesh Yadav over caste mention ban in police documents
UP में जाति का नाम हटाने पर बढ़ा सियासी संग्राम
जातिगत पहचान हटाने का फैसला : सामाजिक समानता या सियासी हथियार?
उत्तर प्रदेश में पुलिस FIR और सरकारी दस्तावेज़ों से जाति हटाने के फैसले ने राजनीति को गरमा दिया है। योगी सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, जबकि अखिलेश यादव इसे सतही सुधार और दिखावा कह रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह आदेश वाकई जातिगत भेदभाव मिटा पाएगा या यह सिर्फ राजनीतिक टकराव का नया मुद्दा बनेगा?
जाति और राजनीति का टकराव
उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से जातिगत समीकरणों के इर्द-गिर्द घूमती रही है। अदालतों के फैसले और सरकारों के निर्णय चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, उनका असर तब तक अधूरा रहता है जब तक वह समाज की गहराई में जमी मानसिकता को नहीं बदल पाते। इलाहाबाद हाईकोर्ट का हालिया आदेश – जिसमें पुलिस की एफआईआर, अरेस्ट मेमो और सरकारी दस्तावेज़ों से जाति हटाने की बात कही गई है – एक तरफ़ संवैधानिक समानता की ओर कदम है, तो दूसरी तरफ़ सियासी घमासान की नई ज़मीन भी बन चुका है।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने तेजी से इस आदेश को लागू करते हुए शासनादेश जारी किया, लेकिन विपक्ष, ख़ासकर समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस निर्णय को सतही और दिखावटी बताया। सवाल यह है कि क्या वाकई यह आदेश समाज से जातिगत भेदभाव मिटा पाएगा, या फिर यह राजनीति का एक और हथियार बनकर रह जाएगा?
आज का शाह टाइम्स ई-पेपर डाउनलोड करें और पढ़ें
हाईकोर्ट का आदेश : संवैधानिक मूल्यों की याद
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 सितंबर को अपने फैसले में साफ़ कहा कि पुलिस दस्तावेज़ों में अभियुक्तों या पीड़ितों की जाति का उल्लेख करना संवैधानिक समानता और नागरिक अधिकारों के खिलाफ़ है। अदालत का तर्क था कि जब संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं, तब सरकारी काग़ज़ात में जाति की पहचान क्यों ज़रूरी है?
अदालत का दृष्टिकोण
संविधान का अनुच्छेद 14, 15 और 21 समानता की गारंटी देते हैं।
जाति का उल्लेख कहीं न कहीं भेदभाव और पूर्वाग्रह को जन्म देता है।
पुलिस रिकॉर्ड और न्यायिक दस्तावेज़ों में जाति की मौजूदगी सामाजिक विभाजन को और मजबूत करती है।
अदालत ने यह भी कहा कि जाति-आधारित महिमामंडन, चाहे वह साइनबोर्ड्स पर हो या वाहनों पर, संवैधानिक आदर्शों के विपरीत है।
योगी सरकार की प्रतिक्रिया : आदेश से शासनादेश तक
सरकार ने बिना समय गँवाए आदेश को लागू करने का निर्णय लिया। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने विस्तृत शासनादेश जारी किया, जिसमें कई बिंदु शामिल थे:
अब एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, अपराध विवरण फॉर्म या अंतिम रिपोर्ट में जाति का ज़िक्र नहीं होगा।
थानों के नोटिस बोर्ड, पुलिस वाहनों और साइनबोर्ड्स से जातिगत संकेत और नारे हटाए जाएंगे।
NCRB के क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) से जाति वाला कॉलम हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी।
व्यक्ति की पहचान पिता के साथ-साथ माता के नाम से होगी।
केवल SC/ST Act जैसे मामलों में कानूनी आवश्यकता के तहत जाति का उल्लेख किया जाएगा।
सरकार ने इसे “समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम” बताया।
विपक्ष का हमला : अखिलेश यादव का सवाल
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस आदेश को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पाँच प्रमुख सवाल उठाए:
क्या यह आदेश 5000 साल पुरानी जातिगत मानसिकता को बदल पाएगा?
वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों में झलकने वाली जाति को मिटाने के लिए क्या कदम होंगे?
नाम से पहले जाति पूछने की प्रवृत्ति कैसे खत्म होगी?
जातिगत भेदभाव जैसे “घर धुलवाना” या सामाजिक बहिष्कार पर सरकार की क्या योजना है?
झूठे आरोप लगाकर जाति के आधार पर बदनाम करने की साजिशों से कैसे निपटा जाएगा?
अखिलेश का कहना है कि सतही बदलावों से समाज में गहरी पैठ बना चुकी जातिवादी सोच खत्म नहीं होगी।
जाति और राजनीति : परंपरा बनाम परिवर्तन
भारत में जाति सिर्फ़ सामाजिक पहचान नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरणों का मूल आधार रही है। उत्तर प्रदेश तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
जाति और चुनाव: यादव, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर और मुस्लिम वोट बैंक हमेशा चुनावी गणित तय करते रहे हैं।
नेताओं का स्टैंड: सत्ता में रहते हुए भी कोई भी सरकार जातिगत समीकरण से मुक्त होकर निर्णय लेने में हिचकती रही है।
अब का विवाद: जाति हटाने का आदेश समाज को बराबरी की ओर ले जा सकता है, लेकिन राजनीतिक दलों को यह अपने वोट बैंक की राजनीति पर सीधा असर डालता हुआ दिख रहा है।
सामाजिक परिप्रेक्ष्य : क्या बदलेगी तस्वीर?
सरकारी आदेश और कागज़ी सुधार ज़रूरी हैं, मगर असली सवाल है – क्या इससे समाज की मानसिकता बदलेगी?
सकारात्मक पहलू
पुलिस रिकॉर्ड्स में जातिगत पूर्वाग्रह की संभावना घटेगी।
न्यायिक प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष दिखेगी।
जातिगत पहचान के बिना नागरिक की पहचान अधिक ‘समान’ मानी जाएगी।
नकारात्मक आशंकाएँ
जमीनी स्तर पर जातिगत भेदभाव की परंपराएँ आसानी से नहीं मिटेंगी।
आदेश का उल्लंघन गुप्त तरीक़े से जारी रह सकता है।
राजनीति में जातिगत रैलियाँ और नारों पर प्रतिबंध लागू कराना कठिन होगा।
कानून बनाम मानसिकता
इतिहास गवाह है कि कानून समाज को दिशा तो दे सकता है, लेकिन मानसिकता बदलना एक लंबी प्रक्रिया होती है। जातिवाद भारतीय समाज की नसों में गहराई तक समाया हुआ है। चाहे वह शादियों में जाति आधारित चयन हो या रोज़गार में रिश्तों का नेटवर्क – यह सोच रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा है।
इसलिए विपक्ष का तर्क है कि केवल आदेश जारी कर देने से जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक इच्छाशक्ति से ठोस बदलाव न लाए जाएं।
राजनीतिक रणनीति : सियासी हथियार या सुधार?
विपक्ष इसे सरकार का “इमेज मेकओवर” बता रहा है। उनके अनुसार, भाजपा इस फैसले को अपने वोट बैंक के लिए उपयोग करेगी। वहीं, सरकार चाहती है कि वह “समानता और न्याय” की संरक्षक के रूप में दिखे।
संभावित असर
भाजपा दलित और पिछड़े वर्गों को यह संदेश देना चाहती है कि वह भेदभाव खत्म करने के पक्ष में है।
विपक्ष को लगता है कि यह केवल “Optics” है, असल मुद्दों पर कोई काम नहीं हो रहा।
जनता के बीच यह विवाद चुनावी माहौल को और गर्माएगा।
निष्कर्ष : सवाल अभी बाकी
जाति हटाने का यह आदेश एक सकारात्मक कदम है, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं। सवाल यह है कि क्या सरकार और समाज मिलकर उस गहरी मानसिकता को बदलने के लिए तैयार हैं, जो सदियों से जातिवाद को जीवित रखे हुए है?
यह आदेश राजनीति में नई बहस ज़रूर पैदा करता है, लेकिन जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए शिक्षा, सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक इच्छाशक्ति – तीनों की आवश्यकता है।