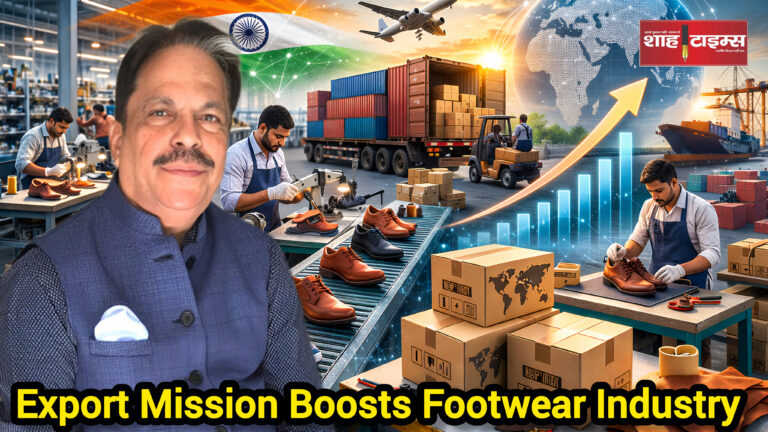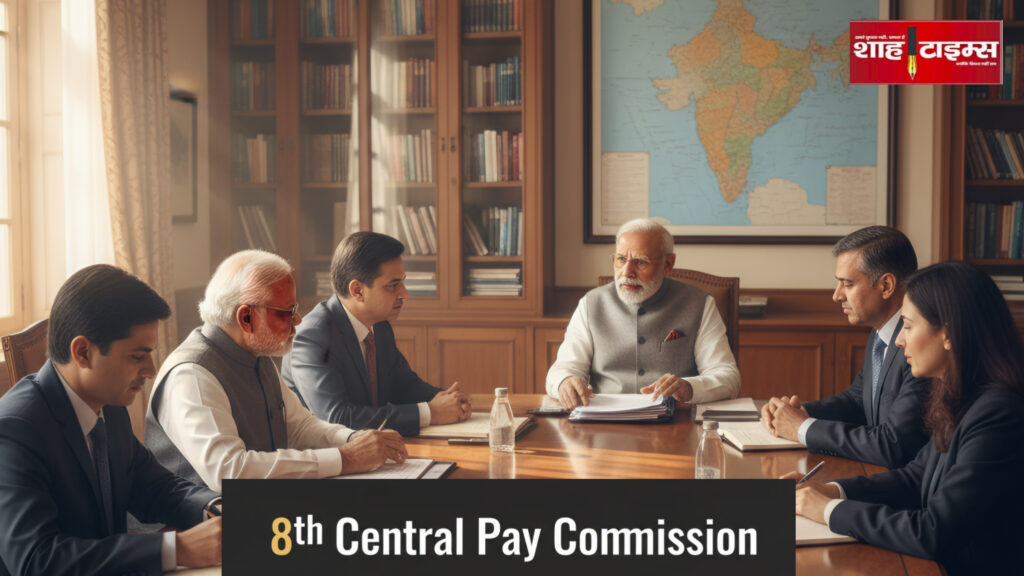
The formation of the 8th Pay Commission was announced in a meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi.
सरकार ने दी 8वें वेतन आयोग को मंज़ूरी, अब उम्मीदें और हक़ीक़त आमने-सामने
📍नई दिल्ली 🗓️ 28 अक्तूबर 2025 ✍️ Asif Khan
केंद्र सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) को औपचारिक मंज़ूरी दे दी है। यह आयोग 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को फ़ायदा पहुँच सकता है। सवाल यह है — क्या वेतन वाकई बढ़ेगा या यह सिर्फ़ एक राजनीतिक घोषणा है?
भारत में वेतन आयोग हमेशा से सरकार और कर्मचारियों के रिश्ते का आईना रहा है। हर दशक के साथ उम्मीदें और हक़ीक़तें बदलती गईं। सातवें वेतन आयोग ने 2016 में लागू होकर एक नया मानक तय किया था, और अब आठवाँ आयोग उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है।
आयोग की संरचना और ज़िम्मेदारी
सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंज़ूरी दी है। यह एक अस्थायी निकाय होगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। अध्यक्ष के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को चुना गया है। सदस्य के रूप में आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष, जबकि सदस्य-सचिव के तौर पर पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को नियुक्त किया गया है।
आयोग का मुख्य काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन ढाँचे की समीक्षा करना है। साथ ही, यह भी देखना होगा कि देश की आर्थिक स्थिति पर इन सिफारिशों का क्या प्रभाव पड़ेगा।
18 महीनों की डेडलाइन और संभावित प्रभाव
सरकार ने आयोग को निर्देश दिया है कि वह अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंप दे। इसका मतलब यह हुआ कि रिपोर्ट लगभग मध्य-2027 तक तैयार हो सकती है। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएँगी।
लेकिन अनुभव बताता है कि भारत में आयोगों की रिपोर्ट अक्सर देरी से लागू होती हैं। सातवाँ वेतन आयोग भी दिसंबर 2015 में रिपोर्ट दे चुका था, मगर लागू 1 जनवरी 2016 से हुआ और कर्मचारियों को संशोधित वेतन कुछ महीनों बाद मिला। इसलिए इस बार भी उम्मीद और इंतज़ार दोनों साथ-साथ चलेंगे।
किसे कितना फ़ायदा?
इस आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स प्रभावित होंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि वेतन में कितनी वृद्धि होगी। इसका जवाब “फिटमेंट फैक्टर” पर निर्भर करेगा — यही वह गणना है जो मूल वेतन को नए मानक में बदलती है।
सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इसका मतलब यह था कि पुराने वेतन को 2.57 से गुणा कर नया बेसिक पे तय किया गया। अगर आठवें आयोग में यह बढ़कर 2.86 या 3.0 हो जाता है, तो कर्मचारियों को काफ़ी लाभ हो सकता है।
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक पे ₹30,000 है, तो 3.0 के फैक्टर से नया बेसिक ₹90,000 तक पहुँच सकता है। हालांकि इसमें महंगाई भत्ता (DA) रीसेट हो जाएगा और नए पैमाने से फिर से शुरू होगा।
डीए और एचआरए का खेल
अभी महंगाई भत्ता 55% तक पहुँच चुका है। नए आयोग के लागू होते ही यह शून्य पर रीसेट हो जाएगा क्योंकि नई सैलरी में महंगाई का असर पहले ही जोड़ दिया जाएगा। इससे शुरुआत में कुल वेतन उतना बड़ा न दिखे, जितना उम्मीद की जा रही है।
एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस भी उसी अनुपात में बदलेगा। मेट्रो शहरों में यह 27% है, जो नई बेसिक पे के हिसाब से फिर से तय होगा। मतलब — सैलरी में सुधार तो होगा, पर साथ में गणना की जटिलताएँ भी बढ़ेंगी।
पेंशनभोगियों के लिए राहत या प्रतीक्षा?
आयोग को पेंशन प्रणाली के वित्तीय पहलुओं पर भी सिफारिशें देने को कहा गया है। खास तौर पर “नॉन-कॉन्ट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम” यानी वह व्यवस्था जिसमें कर्मचारी खुद अंशदान नहीं करते। इस दिशा में सरकार यह देखना चाहती है कि बढ़ती पेंशन लागत को कैसे संभाला जाए।
पेंशनर्स की सबसे बड़ी चिंता यही है कि डीआर (Dearness Relief) कैसे समायोजित होगा। अगर आयोग डीए को बेसिक पे में मर्ज कर देता है, तो शुरू में पेंशन बढ़ेगी, लेकिन आने वाले वर्षों में नई डीआर वृद्धि की गुंजाइश कम हो सकती है।
राज्यों पर असर
राज्य सरकारें अक्सर केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ महीनों बाद अपनाती हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यह प्रभाव एक से दो साल के अंतर से आता है। इसलिए केंद्र के कर्मचारियों की तुलना में राज्यकर्मियों को यह लाभ देर से मिलता है।
यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ राज्य पहले से ही अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार संशोधन लागू करते हैं। ऐसे में आयोग को यह ध्यान रखना होगा कि उसकी सिफारिशें देशव्यापी आर्थिक संतुलन न बिगाड़ें।
क्या यह चुनावी कदम है?
अब सवाल उठता है — क्या यह निर्णय महज़ एक आर्थिक नीति है या राजनीतिक रणनीति?
चूँकि लोकसभा चुनाव 2029 से पहले कोई बड़ा सामाजिक-आर्थिक फैसला सरकार के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस कदम को चुनावी दृष्टि से भी देखा जा रहा है।
केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या भले सीमित हो, लेकिन उनका असर हर राज्य और जिले में दिखाई देता है। रेल, डाक, आयकर, रक्षा, सचिवालय — हर विभाग में इनका नेटवर्क जनता तक पहुँचता है। इसलिए सरकार के लिए यह एक राजनीतिक पूंजी भी है।
आर्थिक अनुशासन बनाम जनसंतोष
यहाँ असली संघर्ष यही है — सरकार को आर्थिक अनुशासन बनाए रखना है और जनता का भरोसा भी।
अगर आयोग बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी सुझाता है, तो वित्तीय घाटा बढ़ सकता है। वहीं अगर सिफारिशें सीमित हों, तो कर्मचारियों में असंतोष।
भारत की GDP ग्रोथ इस समय लगभग 6.8% है, और महंगाई दर 4–5% के बीच। ऐसे में बहुत अधिक वेतन वृद्धि अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकती है। इसलिए आयोग को संतुलन बनाकर चलना होगा — न बहुत उदार, न बहुत कंजूस।
कर्मचारियों की मांगें और संघों का दबाव
Joint Consultative Machinery (JCM) जैसे संगठनों ने पहले ही सरकार को लिखा था कि वे चाहते हैं 50% DA को बेसिक पे में मर्ज किया जाए। इसके अलावा, अंतरिम राहत (Interim Relief) की भी माँग है, ताकि जब तक रिपोर्ट न आए, कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सके।
यह माँग पहली बार नहीं है — हर वेतन आयोग के बीच यह दबाव देखा जाता है। लेकिन सरकार अक्सर कहती है कि अंतरिम राहत तभी मिलेगी जब महंगाई दर असामान्य रूप से बढ़े।
गणना से हक़ीक़त तक
अब ज़रा एक साधारण उदाहरण से समझते हैं —
मान लीजिए किसी कर्मचारी का लेवल-5 का बेसिक पे ₹29,200 है।
वर्तमान डीए 55% यानी ₹16,060
एचआरए 27% यानी ₹7,884
कुल ₹53,144
अगर नया फिटमेंट फैक्टर 2.8 होता है —
नया बेसिक = ₹81,760
डीए = 0% (रीसेट)
एचआरए = ₹22,075
कुल वेतन = ₹1,03,835
यानी लगभग ₹50,000 की वृद्धि दिखेगी, लेकिन असली फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि नया टैक्स-स्लैब और अन्य भत्ते कैसे तय होते हैं।
असली सवाल — कब लागू होगा?
इतिहास बताता है कि रिपोर्ट आने और लागू होने के बीच अक्सर एक साल का अंतर होता है।
अगर रिपोर्ट जून 2027 तक आती है, तो लागू होना संभवतः जनवरी 2028 के आसपास होगा।
इसलिए कर्मचारियों को यह समझना चाहिए कि यह प्रक्रिया तुरंत नहीं, बल्कि क्रमिक है।
मेरा विश्लेषण
एक पत्रकार के तौर पर मेरा मानना है कि यह कदम आवश्यक था। दस साल में एक बार पुनर्मूल्यांकन ज़रूरी है ताकि महंगाई और जीवन-स्तर के बीच संतुलन बना रहे। लेकिन यह भी ज़रूरी है कि आयोग केवल वेतन वृद्धि तक सीमित न रहे — बल्कि उत्पादकता, पारदर्शिता और जनसेवा की गुणवत्ता पर भी विचार करे।
क्योंकि अगर सिर्फ़ पैसे बढ़ें और काम का स्तर न बदले, तो सुधार अधूरा रह जाएगा।
आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग उम्मीदों की नई कहानी लिख सकता है — बशर्ते सिफारिशें व्यावहारिक हों, संतुलित हों और समय पर लागू की जाएँ।
कर्मचारियों को भी यह समझना चाहिए कि सरकार के लिए हर वृद्धि एक आर्थिक चुनौती होती है।यह फैसला न तो सिर्फ़ “गुड न्यूज़” है, न सिर्फ़ “राजनीतिक चाल” — यह दोनों के बीच की एक ज़रूरी कड़ी है।
अब सबकी निगाहें उस रिपोर्ट पर होंगी जो अगले 18 महीनों में आने वाली है।