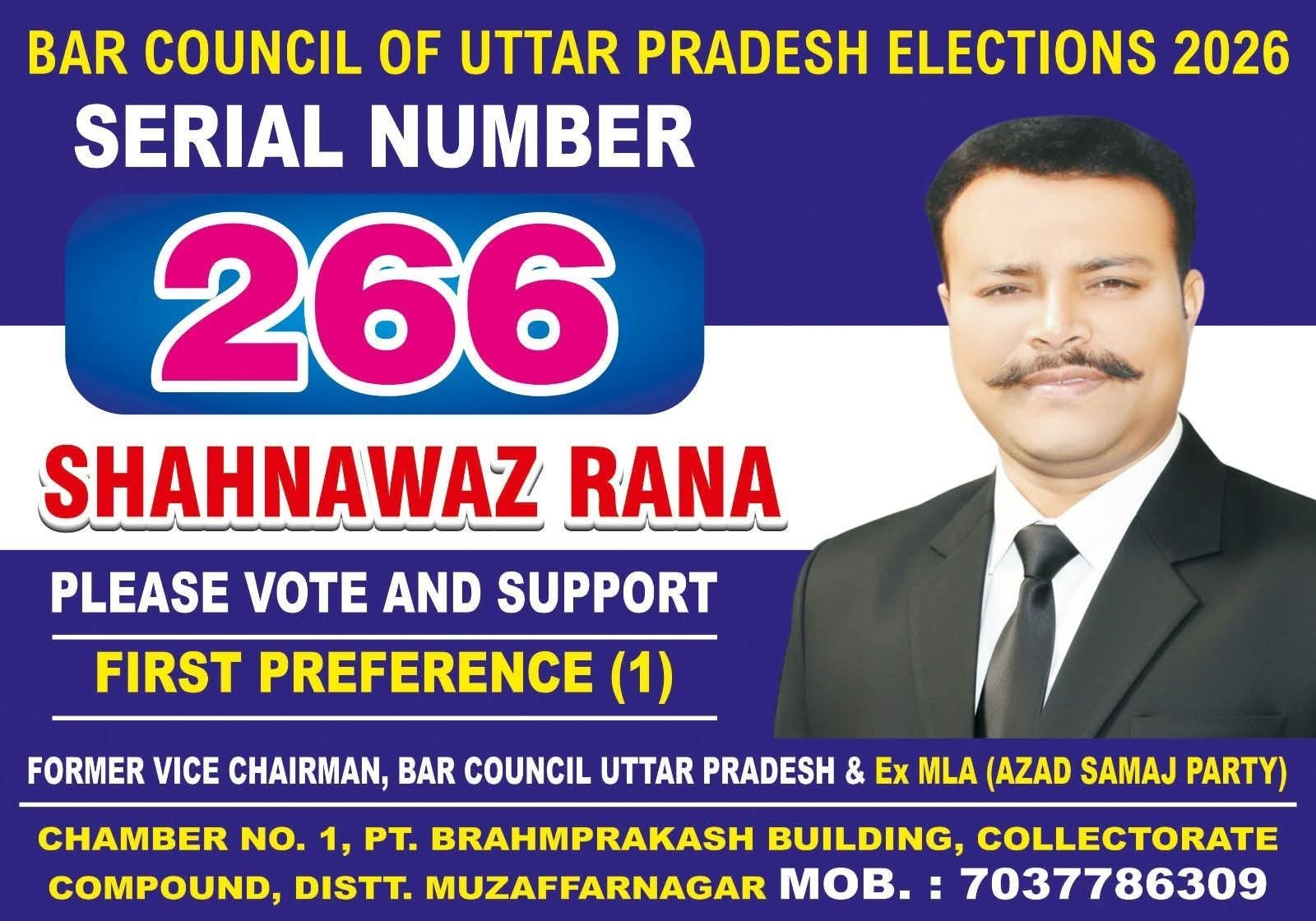From North to South, India’s political landscape remains deeply influenced by dynastic power and family-based leadership.
भारत में राजनीतिक दलों की जड़ें अब विचारधारा से नहीं, बल्कि परिवारों से जुड़ी दिख रही हैं — यही लोकतांत्रिक पतन की असली शुरुआत है।
✍️ एम. हसन
यद्यपि नेहरू-गांधी परिवार के वंशवाद पर चर्चा में हावी है, यह संस्कृति उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व तक, सभी राजनीतिक दलों और क्षेत्रों में पनप रही है। वंशवाद की राजनीति इस हद तक है कि कुछ परिवारों के सदस्य न केवल राजनीतिक विभाजन को पार करते हैं, बल्कि राज्य की सीमाओं को भी पार करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच, न केवल चुनावी राज्य में, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी “वंशवाद की राजनीति” को लेकर बहस शुरू हो गई है।
वंशवाद की राजनीति केवल गांधी-नेहरू परिवार या बिहार में लालू यादव परिवार की पहचान नहीं है, बल्कि यह अब दलीय विभाजन और क्षेत्रीय सीमाओं से परे भारतीय राजनीति का एक अभिन्न अंग बन गई है,लेकिन जबकि नेहरू-गांधी परिवार वंशवाद के बारे में चर्चा में हावी है, यह संस्कृति राजनीतिक दलों और क्षेत्रों में पनपती है-उत्तर से दक्षिण तक, पश्चिम से पूर्व तक। वंशवादी राजनीति इस हद तक है कि कुछ परिवारों के सदस्य न केवल राजनीतिक विभाजन को पार करते हैं, बल्कि राज्य की सीमाओं को भी पार करते हैं। जानकारी से संकेत मिलता है कि देश के 5,294 मौजूदा विधायकों (सांसदों, विधायकों और एमएलसी) में 989 परिवारों के 1174 राजवंश हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और जनता दल (यूनाइटेड), उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा), आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के 25 प्रतिशत से अधिक विधायक राजनीतिक परिवारों से हैं। राष्ट्रीय दलों में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के पास 33.25% राज्य विधानसभाओं और/या संसद में 149 परिवारों के एक से ज़्यादा सदस्य हैं। भाजपा वंशवादी राजनीति को ख़त्म करने का दावा करती है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2024 को लाल किले से कहा था कि “हम वंशवादी राजनीति को ख़त्म कर देंगे”।
लेकिन मौजूदा आँकड़े बताते हैं कि भगवा ब्रिगेड में भी वंशवादी राजनीति की कोई कमी नहीं है। लोकतंत्र को मुट्ठी भर नए ‘लोकतांत्रिक कुलीन वर्गों’ द्वारा नियंत्रित नहीं होने दिया जा सकता, जैसे कि आज वंशवादी राजनीति करने वाले ये राजनीतिक परिवार। वंशवाद की राजनीति सभी राजनीतिक दलों में तेजी से जड़ें जमा रही है। मुद्दा यह है कि वंशवाद की राजनीति के प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है क्योंकि यह निश्चित रूप से निकट भविष्य में खत्म नहीं होने वाली है। इस परिघटना की जांच ब्रिटिश इतिहासकार पैट्रिक फ्रेंच ने अपनी पुस्तक इंडिया- ए पोर्ट्रेट में भी की है। 15वीं लोकसभा के सांसदों के विश्लेषण पर आधारित उनके शोध से कुछ रोचक जानकारियां सामने आई हैं, जैसे कि 100 प्रतिशत सांसद 30 वर्ष से कम आयु के हैं और 31-40 वर्ष आयु वर्ग के 65 प्रतिशत सांसद वंशानुगत सांसद थे। यह परिघटना उस समय भाजपा की तुलना में कांग्रेस में अधिक स्पष्ट थी। इसी प्रकार, उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पूर्व में बिहार और दक्षिण में आंध्र प्रदेश में पारिवारिक राजनीति अन्य राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत है। यह बीमारी धीरे-धीरे वामपंथी दलों में भी फैल रही है, जिन्हें इस प्रवृत्ति का अपवाद माना जाता था, हालांकि पिछले 20 वर्षों में उनका प्रभाव काफी कम हो गया है।
राजनीति में भाई-भतीजावाद और ‘परिवारवाद’ कोई नई बात नहीं है। इसने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, सभी राजनीतिक दलों में, अलग-अलग स्तर पर, जड़ें जमा ली हैं। यह देखते हुए कि प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा उतारे गए अधिकांश उम्मीदवार ‘करोड़पति’ हैं, राजनीतिक दलों के साधारण कार्यकर्ताओं के लिए टिकट पाना मुश्किल होता है। उनकी (करोड़पतियों की) ‘जीतने की संभावना’ भी दूसरों की तुलना में ज़्यादा हो सकती है। आख़िरकार, राजनीतिक दल चुनाव लड़ने और ‘जीतने’ के धंधे में ही लगे रहते हैं। डाले गए वोटों का प्रतिशत और विधायक व सांसद के रूप में चुने गए उम्मीदवार, एक मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल के रूप में उनकी स्थिति और राज्य व/या राजनीतिक दानदाताओं द्वारा दिए गए संसाधनों तक उनकी पहुँच निर्धारित करते हैं।
इस तथ्य को देखते हुए कि 2025 के बिहार चुनावों में भी प्रमुख राजनीतिक दलों की महिला उम्मीदवारों की संख्या लगभग 12 से 14 प्रतिशत के क्षेत्र में बनी हुई है, यह कल्पना करना कठिन है कि राजनीतिक दल 2029 के लोकसभा चुनावों तक 33 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों को कैसे ढूंढ पाएंगे, जब महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 के लागू होने की संभावना है, जब तक कि वे उसी राजनीतिक परिवारों से चुनी गई महिला उम्मीदवारों पर निर्भर न हों।
वंशवाद की राजनीति भी भारत तक ही सीमित नहीं है। 20वीं सदी में अमेरिकी राजनीति में राजनीतिक परिवारों का दबदबा रहा है और आज भी उनका प्रभाव बना हुआ है। यूरोप में भी स्थिति कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। इसलिए, पारिवारिक राजनीति या वंशवाद की राजनीति, बीमारी से ज़्यादा एक लक्षण है।
मुख्य प्रश्न यह है कि भारत में राजनीतिक दल कैसे काम करते हैं और क्या उनमें ‘आंतरिक-दलीय लोकतंत्र’ है। क्या वे सिर्फ़ चुनावी लड़ाइयाँ हैं जो राज्य और राष्ट्रीय चुनावों के समय सक्रिय हो जाती हैं या चुनावों के बीच के समय में भी उनकी कोई भूमिका होती है? क्या राजनीतिक संस्कृति लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए अनुकूल है और क्या पार्टी संगठन पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को मज़बूत करने के लिए तैयार है या सिर्फ़ एक ‘सर्वोच्च’ नेता या ‘आलाकमान’ को आगे बढ़ाने के लिए?
राजनीतिक दलों की भूमिका मोटे तौर पर चुनावी लड़ाई की मशीन तक ही सीमित रही है। नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच संवाद सबसे ज़्यादा चुनावों के समय होता है, जब बूथ स्तर पर मतदाताओं को प्रबंधित करने और बूथ एजेंट व मतगणना एजेंट के रूप में काम करने के लिए कार्यकर्ताओं की सेवाओं की आवश्यकता होती है। नेताओं की चुनावी रैलियों में मतदाताओं को लाने के लिए भी कार्यकर्ताओं की सेवाओं की आवश्यकता होती है। पहले पार्टी कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर पार्टी की ‘आँख और कान’ का काम करते थे। अब यह काम ‘राजनीतिक सलाहकारों’ और सलाहकार फर्मों को सौंप दिया गया है, जो आँकड़ों का विश्लेषण करते हैं, राजनीतिक दलों के लिए आंतरिक सर्वेक्षण करते हैं, उम्मीदवारों के चयन के लिए इनपुट प्रदान करते हैं और चुनावी रणनीति तैयार करते हैं। इन प्रवृत्तियों ने पार्टी कार्यकर्ताओं की संख्या में कमी को और बढ़ा दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं से ज़्यादा, ये ‘पर्दे के पीछे के लोग’ हैं जिनकी पहुँच पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक है।
लगभग सभी राजनीतिक दलों में ‘आलाकमान संस्कृति’ का प्रचलन यह दर्शाता है कि राजनीतिक दल ‘ऊपर से नीचे’ के तरीके से काम करते हैं और शायद ही कोई पार्टी निर्णय नीचे से प्राप्त फीडबैक या सुझावों के आधार पर लिया जाता है।
राजनीतिक दलों में किसी भी संस्थागत तंत्र का अभाव यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक नीति निर्माण में उनकी भूमिका नगण्य बनी रहे। सार्वजनिक नीति को मोटे तौर पर सरकार के अधिकार क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। सत्तारूढ़ दल की भूमिका नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के बजाय सरकार के सभी निर्णयों के समर्थन तक ही सीमित रह जाती है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) देश के 650 से अधिक जिलों में सुसज्जित अत्याधुनिक पार्टी कार्यालयों का निर्माण करने पर गर्व महसूस करती है। ये कार्यालय पार्टी कार्यकर्ताओं को एक सम्मानजनक स्थान प्रदान करने वाले हैं जहाँ वे आ सकते हैं, बैठकें कर सकते हैं और पार्टी नेताओं से मिल सकते हैं। नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी उपकरण पार्टी के सर्वोच्च नेता या पार्टी आलाकमान से हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं तक निर्बाध ‘एकतरफा, ऊपर से नीचे’ संदेश सुनिश्चित करते हैं। हाल ही में, प्रधानमंत्री ने बिहार के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक डिजिटल संवाद किया, क्योंकि राज्य में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। राजनीतिक दलों के कामकाज में ‘आंतरिक-पार्टी लोकतंत्र’ पर अधिक ज़ोर देना वंशवाद की बढ़ती कुप्रथा का एक बेहतरीन समाधान होगा।
(लेखक हिंदुस्तान टाइम्स, लखनऊ में स्टेट ब्यूरो चीफ रहे हैं)