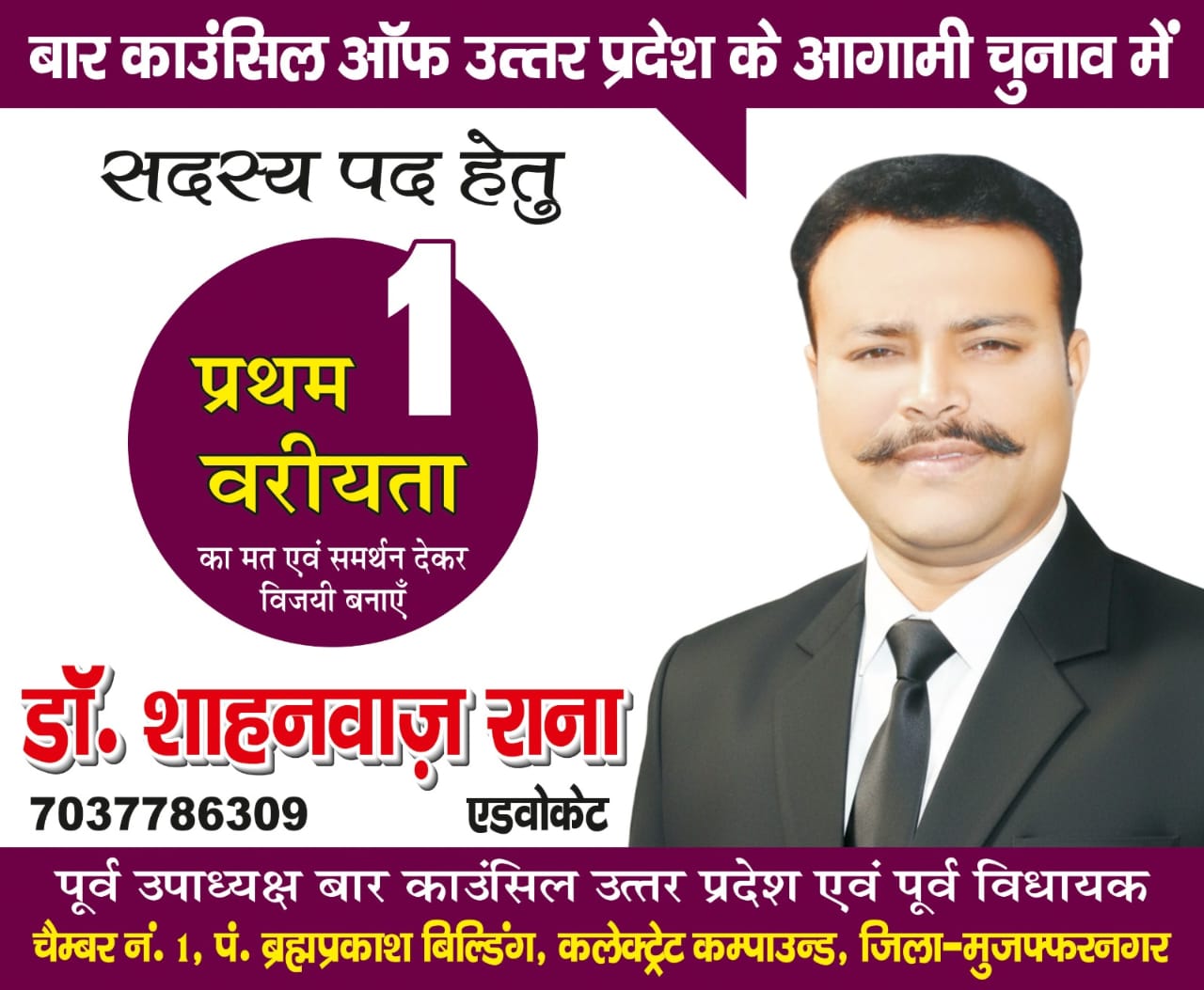ग़ज़ा पर मुस्लिम देशों की एकजुटता — तुर्की की नई कूटनीति की मिसाल
तुर्की की अगुवाई में मुस्लिम दुनिया का ग़ज़ा मिशन – हकीकत या दिखावा?
इस्तांबुल में मुस्लिम देशों की बैठक के बाद ग़ज़ा में शांति के लिए नई पहल — क्या यह उम्मत की एकता है या तुर्की की रणनीतिक चाल? गहराई से पढ़िए इस संतुलित एडिटोरियल विश्लेषण में।
📍Istanbul✍️Asif Khan
मिडिल ईस्ट की हवाओं में एक बार फिर से बारूद और दुआओं की गंध एक साथ तैर रही है। ग़ज़ा के टूटे हुए मकान, बेघर हुए बच्चे और जलती मस्जिदों के मीनार अब सिर्फ एक मानवीय त्रासदी का प्रतीक नहीं रहे — यह पूरी मुस्लिम उम्मत की एक इम्तेहान बन चुकी है। इस्तांबुल से लेकर इस्लामाबाद तक, क़तर से रियाद और जकार्ता तक, मुस्लिम देशों के राजनैतिक गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है — क्या अब ग़ज़ा के लिए कोई “मुस्लिम शांति सेना” बनाई जाएगी? या यह भी राजनीति का एक और दिखावटी मोर्चा बनकर रह जाएगा?
तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यब एर्दोग़ान इन दिनों खुद को इस्लामी दुनिया के “ख़लीफ़ा” की तरह पेश करने की कोशिश में हैं। उनकी विदेश नीति की दिशा साफ़ है — “मुस्लिम एकजुटता के नाम पर क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाना।” इस्तांबुल में हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक ने इसी सोच को ज़मीन पर उतारने की कोशिश की। इसमें क़तर, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन जैसे देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग का मक़सद था — ग़ज़ा में युद्धविराम के बाद की स्थिति पर चर्चा और “पोस्ट-वार स्ट्रक्चर” तैयार करना।
इस्तांबुल मीटिंग – एकता की शुरुआत या एक और बयानबाज़ी?
तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान की मेज़बानी में हुई इस बैठक में ग़ज़ा के हालात पर गहरी चिंता जताई गई। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ग़ज़ा की सुरक्षा और प्रशासन पूरी तरह फिलिस्तीनियों के हाथों में दिया जाए। दिलचस्प यह है कि फिदान ने यह भी दावा किया कि हमास अब प्रशासन फिलिस्तीनियों की एक “कमेटी” को सौंपने को तैयार है।



यह बयान सुनने में तो आशाजनक लगता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संभव है? क्योंकि इज़राइल अब भी ग़ज़ा के कई हिस्सों में सक्रिय है और अमेरिका की मध्यस्थता में जो सीज़फायर हुआ है, वह बेहद नाज़ुक धागे पर टिका है।
फिदान ने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में एक “इंटरनेशनल स्टेबलाइज़ेशन फोर्स” यानी अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल बनाया जा सकता है, जो ग़ज़ा में युद्धविराम की निगरानी करे। पर इसी बिंदु पर भू-राजनीति की परतें खुलने लगती हैं।
क्या यह बल संयुक्त राष्ट्र का विस्तार होगा — या मुस्लिम देशों की अपनी “पीस कीपिंग फोर्स”? अगर दूसरा विकल्प सही है, तो यह पश्चिमी ताक़तों के लिए चिंता का विषय बन सकता है।
मुस्लिम पीस कीपिंग फोर्स — नेक इरादा या रणनीतिक शिफ्ट?
यह विचार नया नहीं है। दशकों पहले भी ओआईसी (ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन) ने ऐसी कोशिशों की थी, लेकिन कभी व्यवहारिक रूप नहीं ले सकी। आज जब तुर्की और क़तर जैसे देश एक नई मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, तो यह सवाल उठना लाज़िमी है कि क्या यह असली एकजुटता है, या केवल तुर्की का प्रभाव बढ़ाने का माध्यम।
क़तर पहले से ही हमास का बड़ा समर्थक रहा है। पाकिस्तान की राजनीतिक इस्लामिक जमातें भी इस कदम को “उम्मत की ताक़त” के तौर पर पेश कर रही हैं। वहीं, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश कुछ हद तक सतर्क हैं। उन्हें डर है कि कहीं यह नई फोर्स तुर्की के नेतृत्व में “पॉलिटिकल इस्लाम” का नया चेहरा न बन जाए।
यानी, एक तरफ ग़ज़ा के लिए हमदर्दी की लहर है, दूसरी तरफ सत्ता के समीकरण बदलने की चाह।
इस्लामिक यूनिटी या इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स
इस्तांबुल की बैठक में सबसे अहम बात यह रही कि हर देश की प्राथमिकता अलग थी। क़तर चाहता है कि उसकी मध्यस्थ भूमिका और बढ़े, पाकिस्तान अपने अंतरराष्ट्रीय इमेज को सुधारना चाहता है, तुर्की नेतृत्व की बागडोर चाहता है, जबकि सऊदी अरब शांति के नाम पर अमेरिका से दूरी कम करना चाहता है।
इन तमाम इरादों के बीच ग़ज़ा का असली दर्द कहीं खो जाता है। ग़ज़ा की गलियों में अब भी बच्चे मलबे में खिलौने ढूंढते हैं, और माताएँ अपनी जानें बचाने के लिए अज़ान के बीच चीख़ती हैं। इस दर्द का कोई धर्म नहीं, लेकिन राजनीति हर जगह मौजूद है।
इज़राइल की चाल और मुस्लिम देशों की बेचैनी
इज़राइल अब भी अपने दायरे का विस्तार करने के लिए आतुर है। वेस्ट बैंक के हिस्से को अपने भीतर मिलाने के लिए एक विधेयक पेश किया जा चुका है। इस्लामिक देशों की बेचैनी का कारण केवल मानवीय नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। अगर ग़ज़ा और वेस्ट बैंक पर इज़राइल का नियंत्रण और मजबूत होता है, तो अरब देशों की सीमाएं और कमजोर हो जाएंगी।
इसीलिए तुर्की और क़तर अब सीधे तौर पर यूएन के शांति मिशन में शामिल होने या नया मिशन शुरू करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि अमेरिका और यूरोप दोनों इस विचार से असहज हैं।
क्योंकि यदि मुस्लिम देशों की संयुक्त फोर्स बनती है, तो यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक “पैरेलल स्ट्रक्चर” तैयार कर देगी — जो नाटो और यूएन की पारंपरिक भूमिका को चुनौती दे सकता है।
पाकिस्तान का रुख – शब्दों से आगे या प्रतीकात्मक?
पाकिस्तान में इस प्रस्ताव पर गहन चर्चा चल रही है। विदेश मंत्री इशाक डार ने भी स्वीकार किया कि ग़ज़ा की स्थिति पर उच्च-स्तरीय विमर्श जारी है। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह वास्तव में सैनिक भेजेगा?
आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के बीच, पाकिस्तान की क्षमता सीमित है। उसके लिए यह कदम अधिक प्रतीकात्मक होगा। फिर भी, घरेलू राजनीति में यह दिखाना कि “हम ग़ज़ा के साथ हैं”, एक भावनात्मक पूंजी है — जिसे हर पार्टी भुनाना चाहती है।
अमेरिका की भूमिका और पश्चिमी मौन
अमेरिका की स्थिति जटिल है। वह एक ओर इज़राइल का सहयोगी है, दूसरी ओर उसे अरब देशों को शांत रखना भी ज़रूरी है। वाशिंगटन के लिए यह मिशन एक नई परीक्षा की तरह है।
यूएन के दायरे में मुस्लिम फोर्स को वैधता देना, अमेरिका के लिए असहज कदम होगा, क्योंकि इससे वेस्ट एशिया में उसका नियंत्रण घटेगा।
यूरोप भी दुविधा में है — एक तरफ मानवाधिकारों की बात, दूसरी तरफ इज़राइल के प्रति राजनीतिक समर्थन।
हमास की स्थिति – हक़ीक़त और गलतफ़हमी के बीच
तुर्की का दावा है कि हमास प्रशासन छोड़ने को तैयार है, लेकिन यह बयान कई विशेषज्ञों के अनुसार एक “डिप्लोमैटिक फ्रेम” भर है।
हमास की हक़ीक़त यह है कि वह खुद को फिलिस्तीनी प्रतिरोध का केंद्र मानता है। उसके लिए प्रशासन छोड़ना, अस्तित्व खोने जैसा है। इसलिए इस पहल का वास्तविक अमल इतना आसान नहीं।
ग़ज़ा और उम्मत – दर्द, सियासत और दुआएँ
हर जुमे को दुनिया भर की मस्जिदों में ग़ज़ा के लिए दुआएँ मांगी जाती हैं। लेकिन यह दुआएँ अब सिर्फ रूहानी नहीं रहीं — इनमें ग़ुस्सा, हताशा और राजनीति सब कुछ घुला है।
मुस्लिम उम्मत के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह ग़ज़ा के लिए एकजुट होकर खड़ी हो पाएगी, या फिर यह भी एक “समीट डिप्लोमेसी” बनकर रह जाएगी।
भारत और वैश्विक प्रतिक्रिया
भारत ने इस मुद्दे पर संतुलित रुख अपनाया है। उसने नागरिकों की सुरक्षा और शांति की अपील की है, लेकिन किसी पक्ष का नाम नहीं लिया। भारत के लिए यह संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि उसकी विदेश नीति “मानवीय और व्यावहारिक” दोनों को साथ लेकर चलती है।
दूसरी ओर, यूरोपीय संघ और यूएन ने भी युद्धविराम की अपील दोहराई है। लेकिन ज़मीन पर हालात जस के तस हैं। ग़ज़ा में अब भी बिजली नहीं, पानी नहीं, और अस्पतालों में दवाएँ ख़त्म हो रही हैं।
नया विश्व समीकरण और उम्मत की परीक्षा
यह कहना गलत नहीं होगा कि ग़ज़ा आज सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुका है — इंसानियत और सत्ता की लड़ाई का प्रतीक।
तुर्की, क़तर, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों की कोशिशें अगर ईमानदारी से की गईं, तो यह इस्लामी दुनिया की नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर इन कोशिशों के पीछे सत्ता और नेतृत्व का लालच है, तो यह एक और धोखा साबित होगा।
मुस्लिम दुनिया की असली ताक़त उसके सैनिक नहीं, उसकी नैतिक आवाज़ है। वही आवाज़, जो कभी क़ुद्स की गलियों में गूँजती थी — “ला इलाहा इल्लल्लाह, फ़लस्तीन की ज़मीं हमारी अमानत है।”
ग़ज़ा के नाम एक सच्ची पुकार
दुनिया के नक्शे पर ग़ज़ा एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन उसकी कहानी इंसानियत के सबसे बड़े सवालों में से एक है।
क्या धर्म, राजनीति और इंसानियत साथ चल सकते हैं?
क्या इस्लामिक देश वाकई एक होकर ग़ज़ा को बचा पाएंगे, या फिर यह भी अंतरराष्ट्रीय मंचों की एक और खोखली आवाज़ बन जाएगी?
जवाब शायद आने वाले महीनों में मिलेगा — लेकिन एक बात साफ़ है,
ग़ज़ा अब सिर्फ फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी उम्मत की इम्तेहान है।