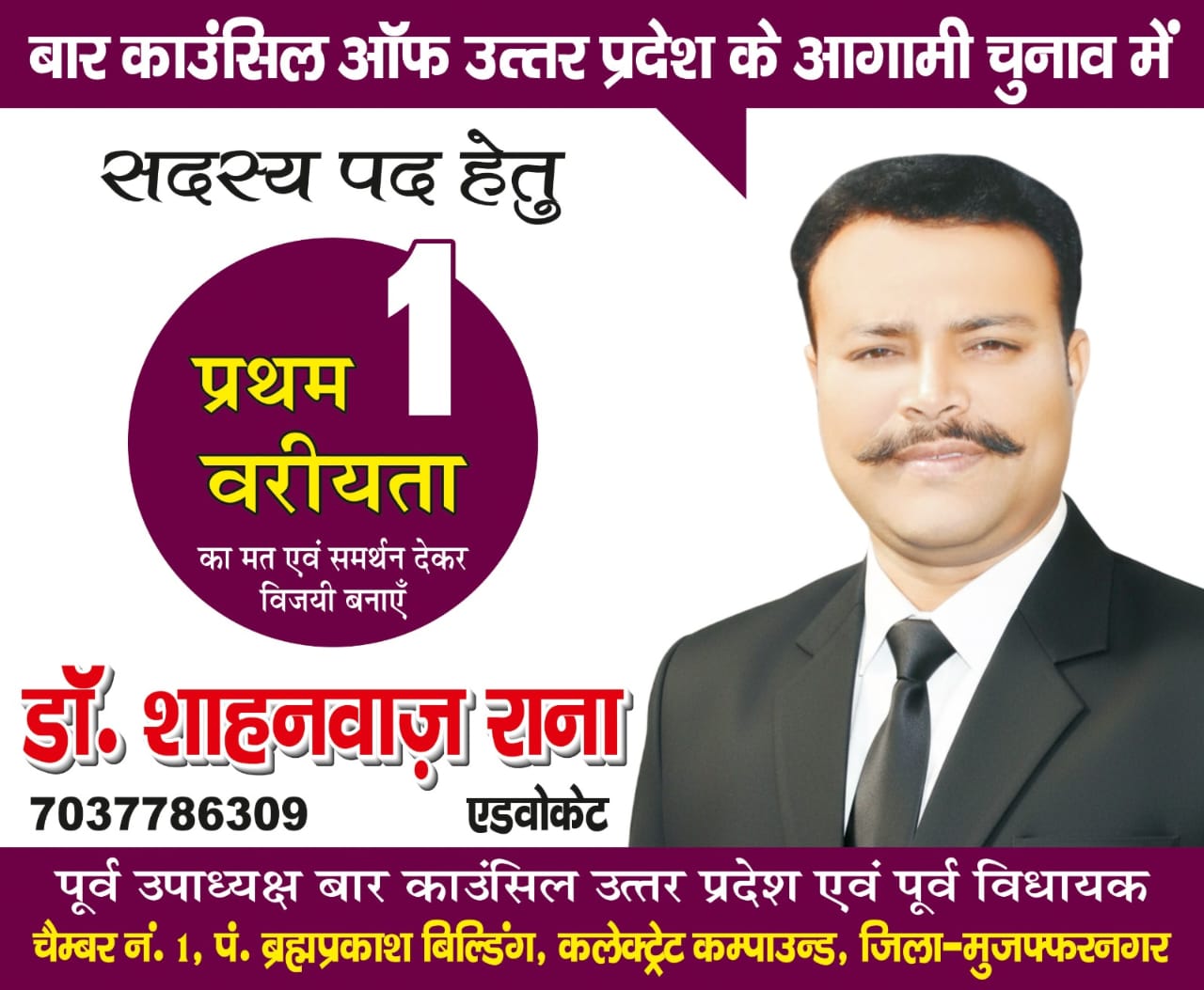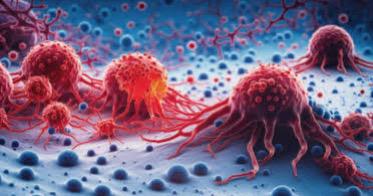Supreme Court order: Remove animals from the road or improve the system — Shah Times Special
सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: अब सड़कों पर न दिखें आवारा जानवर
कुत्ते-मवेशी सड़क पर क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने खींची जवाबदेही
📍 नई दिल्ली
🗓️ 7 नवम्बर 2025
✍️ आसिफ़ ख़ान
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और मवेशियों से बढ़ते हादसों पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी राज्यों को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अदालत ने हाईवे, स्कूलों और अस्पतालों से जानवरों को हटाने, हेल्पलाइन शुरू करने और स्थायी आश्रय गृह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा है, बल्कि मानवीय जिम्मेदारी और प्रशासनिक सुस्ती का आईना भी है।
हाईवे पर जानवर खतरा नहीं, इंसानों की जिम्मेदारी
भारत में “आवारा जानवर” शब्द अब सिर्फ़ दया या डर का विषय नहीं रहा, बल्कि यह समाज और शासन—दोनों की असफलताओं का प्रतीक बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश इसी गहराई को छूता है। अदालत ने साफ़ कहा — “सड़क पर न इंसान असुरक्षित रहें, न जानवर बेसहारा।”
यह बात जितनी कानूनी लगती है, उतनी ही नैतिक भी है।
अदालत का निर्देश और उसका अर्थ
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राजस्थान हाई कोर्ट के अगस्त आदेश को दोहराते हुए कहा कि सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से मवेशियों को तुरंत हटाया जाए।
“पेट्रोल टीम्स 24×7 सक्रिय रहें, हेल्पलाइन नंबर प्रमुखता से लगाए जाएं, और सड़क से हटाए गए मवेशियों को वापस न छोड़ा जाए,” — यह आदेश महज़ प्रशासनिक नहीं, बल्कि नीति-निर्माण की दिशा में चेतावनी है।
सवाल उठता है — क्या यह आदेश लागू हो पाएगा?
भारत में नीतियाँ बनती बहुत हैं, पर ज़मीन पर टिकती कम हैं। मवेशियों को हटाना आसान नहीं क्योंकि वे सिर्फ़ “जानवर” नहीं, बल्कि कई परिवारों की आजीविका का हिस्सा हैं।
मवेशी और समाज का संबंध
गाँव से लेकर शहर तक, गाय और बैल सिर्फ़ धार्मिक प्रतीक नहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी हैं। जब खेत घटे, तो चराई के लिए ज़मीन कम हुई, और ये जानवर सड़कों पर आ गए।
क़ानून कहता है कि सड़कों पर इन्हें रखना अपराध है, पर ग़रीबी कहती है — “घर कहाँ दें?”
इस टकराव में न सरकार ने ठोस समाधान दिया, न समाज ने वैकल्पिक रास्ता चुना।
इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि “सड़क से हटाओ”, तो ज़रूरी है कि साथ में यह भी कहा जाए — “कहाँ रखो।”
आवारा कुत्तों पर अदालत का नया दृष्टिकोण
दिल्ली-एनसीआर से लेकर छोटे कस्बों तक, कुत्तों के हमलों की घटनाएँ बढ़ी हैं। अदालत ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सरकारी दफ्तरों की फेंसिंग अनिवार्य की जाए ताकि कुत्ते अंदर न घुसें।
वकील ननिता शर्मा ने अदालत के आदेश पर भावनात्मक प्रतिक्रिया दी — “ये बेजुबान हैं, सज़ा क्यों मिल रही है?”
उनकी बात में दर्द है, लेकिन अदालत के पास आँकड़े हैं —
हर साल 1.6 करोड़ लोग देश में कुत्तों के काटने से प्रभावित होते हैं। कई मामलों में बच्चे, बुज़ुर्ग और गर्भवती महिलाएँ शामिल हैं।
यह आँकड़ा करुणा से ज़्यादा कार्रवाई माँगता है।
कानूनी और मानवीय संतुलन
यह बहस अब “कुत्ता प्रेम बनाम इंसान की सुरक्षा” तक सीमित नहीं रह गई है।
कानून कहता है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियमों के तहत कुत्तों को बिना कारण दूसरी जगह ले जाना मना है। पर जब खतरा बढ़े, तो अदालत कहती है — “मानव जीवन पहले।”
यह संतुलन कठिन है।
इस्लामी समाज में भी हदीसें कहती हैं — “हर जीव की हिफ़ाज़त रहम का हिस्सा है।”
और हिन्दू परंपरा में — “सर्वे भवन्तु सुखिनः।”
पर न्यायशास्त्र में प्राथमिकता उस जीवन को दी जाती है जो खतरे में है।
इसलिए अदालत की दृष्टि में — “सुरक्षा पहले, करुणा बाद में।”
राजमार्गों की सच्चाई
कहना आसान है — “NHAI मवेशियों को हटाए।”
पर जो ड्राइवर रोज़ दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे या जयपुर हाइवे से गुजरते हैं, वे जानते हैं कि गोधन अब खतरा बन चुका है। रात में अचानक सड़क पर आए पशु से टकराव, और फिर एक ज़िंदगी खत्म।
सरकारी डेटा कहता है कि हर साल लगभग 5,000 से ज़्यादा सड़क हादसे आवारा जानवरों की वजह से होते हैं।
क्या यह सिर्फ़ प्रशासन की गलती है? नहीं।
यह हम सबकी लापरवाही का नतीजा है — जब हम सड़क किनारे दूध पिलाकर खुद को दयालु समझ लेते हैं, लेकिन वही जानवर अगले दिन किसी ट्रक के नीचे आ जाता है।
शहरी बनाम ग्रामीण नैतिकता
ग्रामीण समाज में जानवर “घर का हिस्सा” हैं, जबकि शहर में “परेशानी।”
यह विभाजन मानसिकता का है, न कि वास्तविकता का।
शहरों में जब लोग कुत्तों को सोसायटी में खाना खिलाते हैं, तो दूसरा वर्ग कहता है — “यह खतरा है।”
यह वही समाज है जो कभी गाय को माँ कहता था, अब कार की बॉडी पर खरोंच देखकर शिकायत दर्ज कराता है।
अदालत ने इसी दोहरेपन को रेखांकित किया —
“प्रेम हो तो नियमों में हो, न कि अराजकता में।”
शेल्टर हाउस और बर्थ कंट्रोल
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कुत्तों को शेल्टर में भेजा जाए और वहीं रखा जाए।
पर शेल्टर हाउस की हालत देश में कैसी है, यह किसी से छिपा नहीं। कई जगह न दवा है, न खाना, न स्टाफ।
अगर इंसानों के अस्पतालों में ही व्यवस्था बदहाल है, तो जानवरों के लिए व्यवस्था कौन बनाएगा?
यही वह जगह है जहाँ सरकार और सिविल सोसाइटी को साथ आना होगा।
म्यूनिसिपल बॉडीज़ को सिर्फ़ आदेश नहीं, फंड और मॉनिटरिंग दोनों चाहिए।
Animal Welfare Board को एक्टिव किया जाए, NGOs को जवाबदेह बनाया जाए।
और सबसे ज़रूरी — शहरी नागरिकों को संवेदनशील बनाना।
आलोचनात्मक दृष्टि
कई एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश करुणा के खिलाफ़ है।
पर अगर आदेश न दिया जाता, तो क्या होता?
हर महीने 100 से ज़्यादा डॉग-बाइट केस सिर्फ़ दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आते हैं।
एक छोटी बच्ची की मौत के बाद ही समाज को जागरूकता आती है, फिर भूल जाता है।
कानून का काम है — जागरूकता को बाध्यता बनाना।
फिर भी, अदालत को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्रवाई “क्रूरता” में न बदले।
जानवरों की सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी मानव जीवन की।
इसीलिए यह आदेश दोहरी चेतावनी है — इंसान भी संभले, शासन भी।
आगे का रास्ता
1️⃣ हर जिले में “Animal Task Force” बनाई जाए, जो ट्रैफिक पुलिस और नगर निकाय के साथ समन्वय करे।
2️⃣ शेल्टर हाउसों का स्टैंडर्ड तय हो — फ़ूड, वैक्सीन, मेडिकल चेकअप और मॉनिटरिंग अनिवार्य।
3️⃣ स्कूलों में बच्चों को “एनिमल सेंसिटिविटी” की शिक्षा दी जाए।
4️⃣ मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स को भी अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी — प्यार का प्रचार तभी अर्थपूर्ण है जब वह सुरक्षा से जुड़ा हो।
नतीजा
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश महज़ एक फैसला नहीं, एक दर्पण है —
जो हमें दिखाता है कि हमने “सभ्यता” के नाम पर कितनी असभ्यता को सामान्य बना लिया है।
सड़क पर मवेशी, कॉलोनी में कुत्ते, और शासन में चुप्पी — यह सब विकास का नहीं, विफलता का चित्र है।
अब ज़रूरत है “आदेश” की नहीं, “अनुशासन” की।
करुणा और क़ानून दोनों का संतुलन ही भारत की असली पहचान बनेगा।