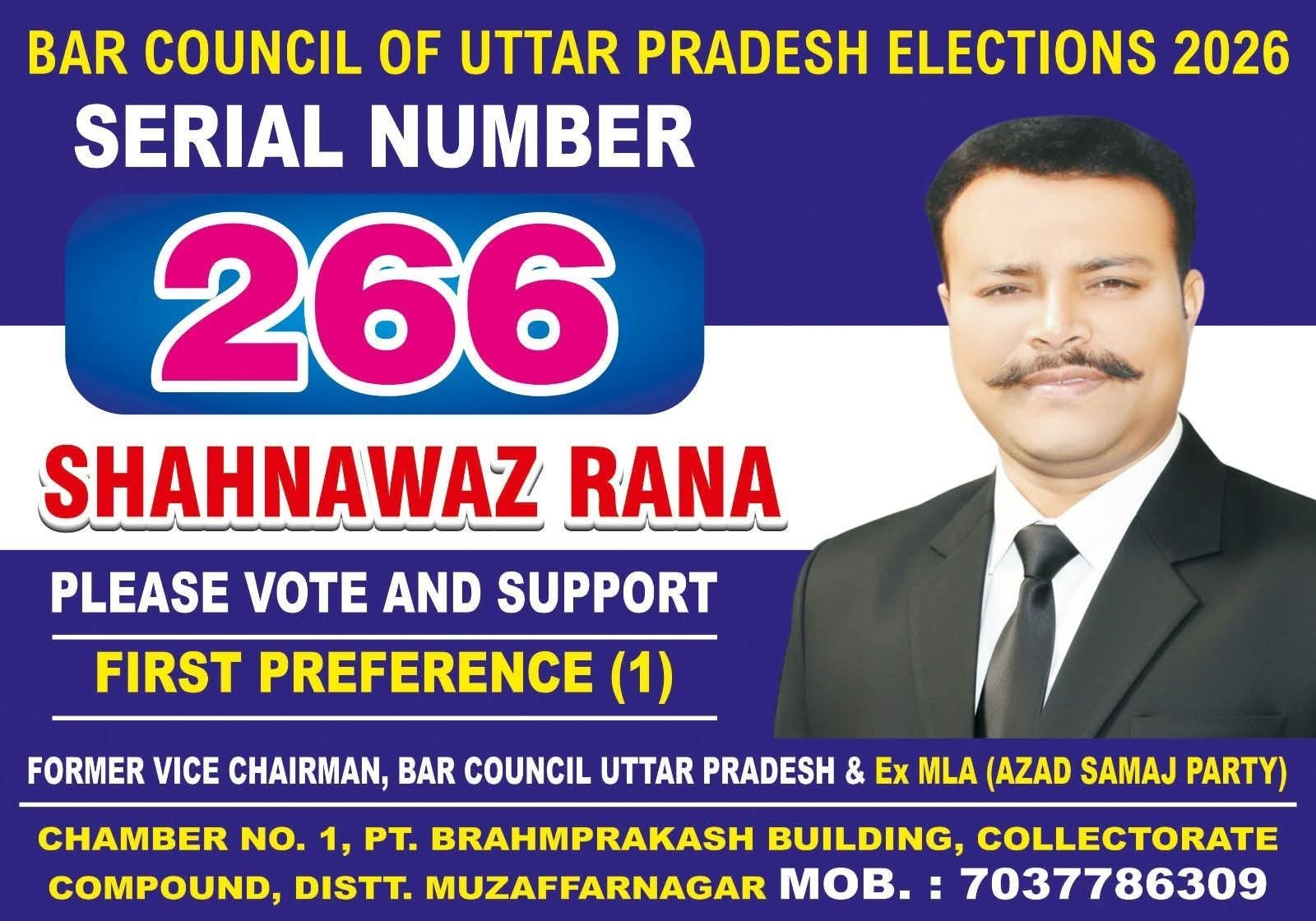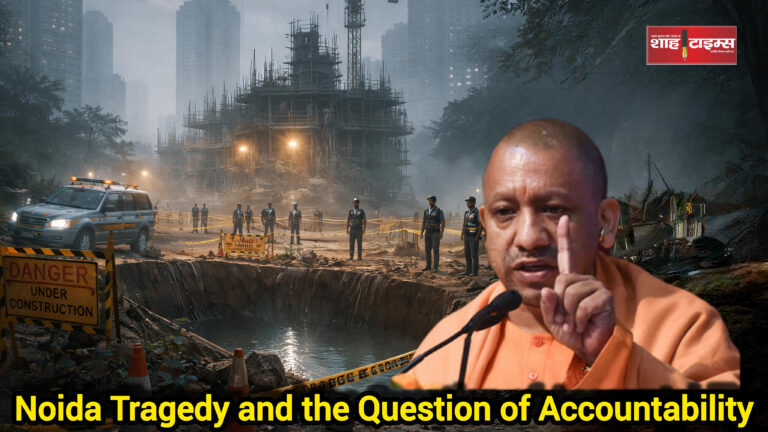Supreme Court building front view with judges in discussion, representing withdrawal of remarks against Allahabad High Court judge – Shah Times
CJI के पत्र के बाद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, HC जज पर सख्त टिप्पणी वापस
इलाहाबाद हाईकोर्ट जज मामले में सुप्रीम कोर्ट की सफाई, आदेश का विवादित हिस्सा हटाया
सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट जज जस्टिस प्रशांत कुमार पर की गई सख्त टिप्पणी वापस ली। जानिए क्यों कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव किया और इस पर न्यायिक प्रणाली के लिए क्या संदेश गया।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम: इलाहाबाद हाईकोर्ट जज पर टिप्पणी वापस
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम कदम उठाते हुए 4 अगस्त 2025 को दिए गए अपने आदेश के विवादित हिस्से को वापस ले लिया। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ था, जिसमें उन्हें रिटायरमेंट तक आपराधिक मामलों के रोस्टर से हटाने और वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ डिवीजन बेंच में बैठाने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य जज को शर्मिंदा करना नहीं था, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना था।
यह कदम न केवल न्यायिक मर्यादा को लेकर एक मिसाल है, बल्कि यह इस सवाल को भी जन्म देता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर आंतरिक न्यायिक प्रतिक्रिया और पुनर्विचार की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए।
मामला कैसे शुरू हुआ
4 अगस्त को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने एक दीवानी विवाद में आपराधिक कार्यवाही बनाए रखने के आदेश को लेकर जस्टिस प्रशांत कुमार की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह के निर्णय न्यायिक तर्कशक्ति पर सवाल उठाते हैं और इस कारण जस्टिस कुमार को आपराधिक रोस्टर से हटाने का निर्देश दिया गया था।
इस आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के कम से कम आठ जजों ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर विचार किया जाए। यहां तक कि हाईकोर्ट में यह मांग उठी कि आदेश को मानने से इनकार किया जाए। मामला धीरे-धीरे न्यायपालिका के भीतर संवैधानिक टकराव का रूप लेने लगा।
CJI का हस्तक्षेप
स्थिति तब बदली जब मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ (CJI) ने जस्टिस पारदीवाला को पत्र लिखकर आदेश पर पुनर्विचार करने को कहा। CJI ने संकेत दिया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हाईकोर्ट के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में सीधे हस्तक्षेप जैसा प्रतीत हो सकता है।
न्यायपालिका में यह सिद्धांत स्थापित है कि “चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ रोस्टर” होते हैं। यानी किस जज को कौन-सा मामला सुनना है, यह पूरी तरह से कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी शुक्रवार को अपने संशोधित आदेश में इस सिद्धांत को दोहराया।
SC की सफाई – गरिमा बनाम व्यक्तिगत आलोचना
सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में स्पष्ट किया कि 4 अगस्त का फैसला व्यक्तिगत आलोचना के लिए नहीं था।
जस्टिस पारदीवाला ने सुनवाई में कहा:
“हमारा उद्देश्य किसी जज को शर्मिंदा करना नहीं है। लेकिन जब मामला कानून के शासन को प्रभावित करता है, तो यह न्यायालय सुधारात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य होता है।”
यह बयान न्यायिक अनुशासन और व्यक्तिगत गरिमा के बीच संतुलन बनाने का प्रयास था।
आज का शाह टाइम्स ई-पेपर डाउनलोड करें और पढ़ें
हाईकोर्ट के भीतर की नाराज़गी
इलाहाबाद हाईकोर्ट के भीतर इस आदेश के खिलाफ असंतोष का माहौल था। कई जजों का मानना था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से हाईकोर्ट की स्वायत्तता पर चोट पहुंचती है। न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा के नेतृत्व में भेजे गए पत्र पर सात अन्य जजों ने भी हस्ताक्षर किए थे।
यह पहली बार नहीं है जब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच प्रशासनिक क्षेत्राधिकार पर बहस हुई हो। लेकिन इस बार मामला सीधे-सीधे एक नामित जज के कार्यक्षेत्र को सीमित करने से जुड़ा था, जिसने इसे संवेदनशील बना दिया।
संतुलन की ज़रूरत
इस पूरे प्रकरण से तीन बड़े सवाल उभरते हैं:
क्या सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट जज की कार्यसूची तय करने का अधिकार है?
– संवैधानिक ढांचे में यह अधिकार मुख्य न्यायाधीश (हाईकोर्ट) के पास है। SC का हस्तक्षेप अपवादस्वरूप होना चाहिए।
क्या सार्वजनिक आलोचना से न्यायिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है?
– हां, क्योंकि जज भी इंसान हैं और उनकी सार्वजनिक छवि का असर उनके न्यायिक कार्य पर पड़ सकता है।
क्या आंतरिक संवाद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी?
– बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के बजाय पहले CJI स्तर पर आपसी बातचीत से मामला सुलझाया जा सकता था।
कानून के शासन का सवाल
जस्टिस पारदीवाला ने टिप्पणी की कि अगर कानून का शासन अदालतों के भीतर ही कमजोर हो गया, तो देश में न्याय व्यवस्था का ढांचा ढह जाएगा। यह बात सही है, लेकिन इसे लागू करते समय यह भी देखना होगा कि कार्रवाई का तरीका न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ न हो।
राजनीतिक और कानूनी महत्व
हालांकि यह मामला राजनीतिक नहीं है, लेकिन इसके कानूनी मायने गहरे हैं। यह घटना दिखाती है कि भारतीय न्यायपालिका के भीतर भी जवाबदेही, सम्मान और अधिकार-सीमा के बीच खींचतान मौजूद है।
इसके अलावा, यह मिसाल आने वाले समय में कई मामलों में संदर्भ के रूप में पेश की जा सकती है—खासकर तब, जब उच्चतम न्यायालय को लगता है कि किसी उच्च न्यायालय का आदेश न्यायिक मर्यादा के अनुरूप नहीं है।
सुधारात्मक न्याय बनाम संस्थागत स्वतंत्रता
सुप्रीम कोर्ट का आदेश वापस लेना इस बात का संकेत है कि संस्थागत स्वतंत्रता को बनाए रखना न्यायिक सुधार का भी हिस्सा है। अगर शीर्ष अदालत यह स्वीकार करती है कि कुछ टिप्पणियां वापस ली जानी चाहिएं, तो यह न्यायिक विनम्रता का उदाहरण है।
यह घटना आने वाले समय में भारत की न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी साबित हो सकती है, जहां मर्यादा, अधिकार और गरिमा—तीनों का संतुलन साधना ही असली चुनौती है।
Supreme Court revises August 4 order on Allahabad HC judge