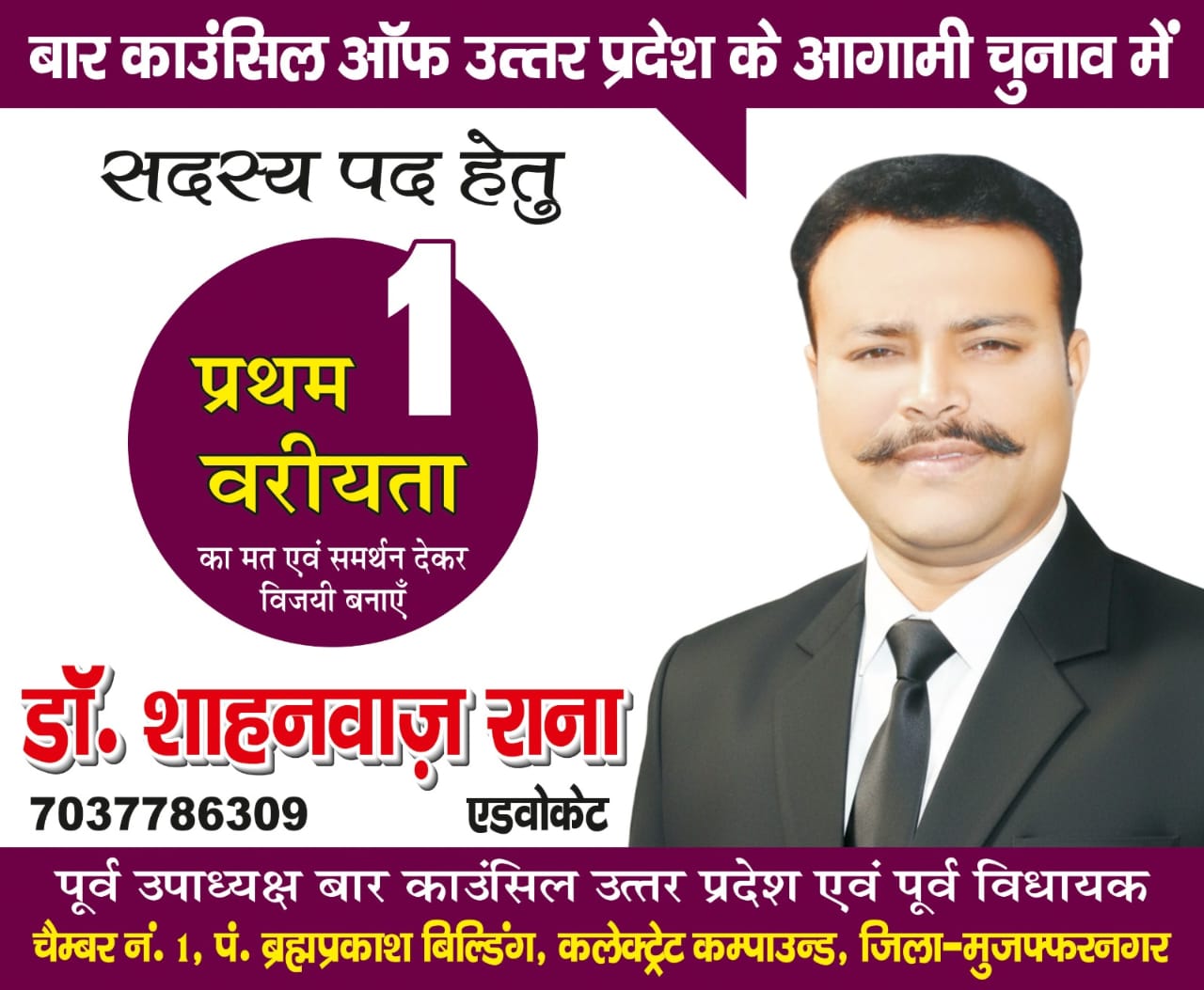Muzaffarnagar DAV College protest scene representing justice demand
फीस विवाद से मौत तक: उज्ज्वल राणा केस में सियासी और कानूनी सवाल
📍मुज़फ़्फ़रनगर |🗓️ 11 नवंबर 2025 | ✍️ आसिफ़ ख़ान
मुज़फ़्फ़रनगर के बुढ़ाना स्थित डीएवी पीजी कॉलेज में बी.ए. छात्र उज्ज्वल राणा की आत्मदाह से हुई मौत की मुकम्मल पड़ताल पेश करता है। इसमें संस्थागत लापरवाही, पुलिस की दखलअंदाज़ी, फीस वसूली में ज़बरदस्ती, प्रत्यक्ष उकसाहट और जवाबदेही के ढांचे की नाकामी को शाह टाइम्स एडिटोरियल में गहराई से समझा गया है।
उज्ज्वल राणा केस: संस्थागत ज़ुल्म, पुलिस की भूमिका और न्याय की जद्दोजहद
मुज़फ़्फ़रनगर की हवा इन दिनों बोझिल है। शहर की गलियों में एक बेचैन ख़ामोशी तैरती है, जैसे हर आदमी अपनी ज़बान के पीछे एक सवाल दबा रहा हो: क्या सचमुच बीए के छात्र की ज़िंदगी ₹5,250 के बकाये के बोझ तले ख़त्म हो सकती थी? यह सवाल सिर्फ़ जज़्बाती नहीं है, बल्कि इस समाज, हमारे तालीमी निज़ाम और राज्य मशीनरी की बुनियादी नाकामी पर सीधी चोट है। उज्ज्वल राणा की मौत सिर्फ़ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि उस संस्थागत ज़ुल्म की मिसाल है जिसके ख़िलाफ़ आज के नौजवान लगातार लड़ रहे हैं, फिर भी बार-बार हारते हुए नज़र आते हैं।
उज्ज्वल राणा की कहानी पहली नज़र में एक मामूली फ़ीस विवाद जैसी लग सकती है। लेकिन जब आप इस केस की तह में जाते हैं, तो यह मामूली नहीं—बल्कि एक संगठित दमन की साजिश जैसा महसूस होता है। कॉलेज प्रशासन का रवैया, प्रिंसिपल प्रदीप कुमार की कथित हिंसा, और पुलिस की दखलअंदाज़ी—तीनों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें एक होनहार और समझदार नौजवान की उम्मीद पूरी तरह टूट गई।
लोग कहते हैं कि उज्ज्वल शांत स्वभाव का लड़का था। लोग यह भी बताते हैं कि वह मेहनती था, दूसरों की मदद करता था, और गरीब छात्रों की आवाज़ बनने की कोशिश करता था। यही बात शायद उसे कॉलेज प्रशासन की नज़रों में “मुसीबत का लड़का” बना गई। तालीमी संस्थान जहां खुलेपन, सहानुभूति और बातचीत की जगह होने चाहिए, वहीं वे अक्सर अपनी सत्ता को बचाने के लिए हर आवाज़ को दबाने लगते हैं। इस मसले में भी ऐसा ही हुआ।
₹7,000 की कुल फीस में से मात्र ₹1,750 जमा करने के बाद बकाया ₹5,250 का विवाद कोई पहाड़ जैसी समस्या नहीं थी। मगर जिस तरह प्रशासन ने इस रकम को वसूलने के लिए अपमान, गाली-गलौज, बाल खींचने, पिटाई और धमकियों का सहारा लिया, वह किसी भी सभ्य समाज में अकल्पनीय है। “ज़ुल्म जब हद से बढ़ जाए तो इंसान का सब्र जवाब दे देता है।” यही सब्र उज्ज्वल का भी जवाब दे गया।
यहां मेरा सवाल मुश्किल और करारा है: क्या सिर्फ़ ₹5,250 की रकम वसूलने के लिए किसी प्रिंसिपल को यह हक़ है कि वह छात्र की पिटाई करे? क्या तालीमी इदारे ऐसे चलाए जाते हैं कि फीस नहीं भरी तो पहले धमकी, फिर पुलिस बुलाओ, और आख़िर में अपमान कर दो?
पुलिस की भूमिका तो और भी परेशान करने वाली है। यह कोई अपराध की जांच नहीं थी; यह कॉलेज और पुलिस का एक अनौपचारिक गठजोड़ था। यह वही पुलिस है जिसका काम नागरिकों की हिफ़ाज़त करना है। लेकिन यहाँ आरोप है कि उन्होंने कॉल पर आते ही छात्र को धमकाया और पीटा। “जिस पर हाथ होना चाहिए था, उसी के हाथ में हथकड़ी थी।”
और फिर वह वाक्य—जो पूरे घटना क्रम को अपराध की श्रेणी में धकेल देता है—जब उज्ज्वल ने अपनी जान लेने की धमकी दी, तो प्रिंसिपल और पीटीआई ने कथित तौर पर कहा: “कल करता हो तो आज कर ले।” यह सिर्फ़ क्रूरता नहीं, यह अपराध की सक्रिय प्रेरणा है। कानून की भाषा में इसे instigation कहते हैं, और यह धारा 306 का साफ़ मामला बनता है।
मैं यहाँ एक चुनौतीपूर्ण सवाल उठाता हूँ: बहुत से मामलों में आरोपी यही दलील देते हैं कि उनकी बात को गलत समझा गया, उनका इरादा नहीं था। लेकिन क्या ऐसा बयान किसी भी तर्क में “ग़लतफ़हमी” कहा जा सकता है? नहीं। इंसान जब संकट में हो, उसकी मानसिक हालत कमज़ोर हो, तब एक प्रभारी अधिकारी का यह कहना—सीधी उकसाहट है।
यहीं सबसे ज़्यादा अमानवीय पहलू सामने आता है: जब उज्ज्वल खुद को आग लगा चुका था, तो प्रिंसिपल और पीटीआई ने कथित तौर पर जो छात्रों को चेतावनी दी—“जो बचाने आएगा, उसे निलंबित कर देंगे”—वह सिर्फ़ अपराध की चूक नहीं, बल्कि अपराध की साज़िश जैसा महसूस होता है। इस डिग्निटी-किलिंग को देखने वाले छात्र खुद आग में कूद पड़े, उनके हाथ और बैग जल गए। मगर संस्थागत सत्ता ने उन्हें रोका। “जुर्म के सामने ख़ामोशी भी जुर्म होती है।”
अब अगर आप इस केस की कानूनी स्थिति देखें, तो एफआईआर में प्रिंसिपल, प्रबंधन, पीटीआई और तीन पुलिसकर्मियों को नामजद किया गया है। लेकिन यह नामजदगी भी उस वक्त हुई जब सोशल मीडिया पर ग़ुस्सा उबल पड़ा, सड़कें भर गईं, धरना हुआ, भीड़ इकट्ठा हुई। यानी संस्थागत कार्रवाई अपने-आप नहीं, बल्कि दबाव में हुई। यह राज्य की उस कमजोरी की निशानी है जिसके चलते आम जनता को न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है।
सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ़ एक कॉलेज का मामला है? नहीं। यह पूरे तालीमी ढांचे पर सवाल उठाता है। भारत में बहुत से कॉलेज और स्कूल फीस वसूली को सत्ता का हथियार बना लेते हैं। उन्होंने शिक्षा को सेवा नहीं, कारोबार बना दिया है। फीस नहीं भरी, तो परीक्षा रोक दो, नाम काट दो, अपमान करो—यह मॉडल हर दिन हजारों छात्रों को दबाव में डालता है। यह वही व्यवस्था है जो गरीब छात्रों को बाहर धकेलती है, अमीरों के लिए जगह बनाती है, और दबाव में आकर छात्रों को मानसिक संकट में डालती है।
सवाल उठता है—क्या कोई ऐसा सिस्टम है जिससे शिकायत सुनी जा सके? इस केस में तो साफ़ है कि शिकायत निवारण तंत्र मौजूद ही नहीं था। कॉलेज प्रशासन के ख़िलाफ़ शिकायत करना ही छात्र के लिए जोखिम बन गया। जो आवाज़ उठाता, वही निशाना बन जाता।
“जहाँ आवाज़ दबा दी जाए, वहाँ इंसाफ़ का दरवाज़ा बंद हो जाता है।” यही हाल यहाँ हुआ।
कानून के लिहाज से देखें, तो धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) का जो मुक़द्दमा दर्ज हुआ है, वह मजबूत दिखता है। क्योंकि instigation, harassment, humiliation और physical assault—ये सारे तत्व स्पष्ट रूप से मौजूद हैं। और जब कोई अधिकारी छात्रों को बचाने से भी मना करे, तो यह अपराध और कठोर हो जाता है।
अब मैं एक counterpoint भी पेश करता हूँ—कभी-कभी संस्थान यह कहते हैं कि छात्र मानसिक रूप से कमज़ोर था, या वह तनाव नहीं झेल पाया। लेकिन यह तर्क न केवल कमज़ोर है, बल्कि क्रूर भी है। किसी भी युवा छात्र के मानसिक स्वास्थ्य की ज़िम्मेदारी संस्था पर भी होती है। और जब संस्था खुद उत्पीड़न करे, तो वह “कमज़ोरी” का तर्क एक बचने की कोशिश लगती है।
उज्ज्वल राणा। के अंतिम शब्द “इंसाफ़… इंसाफ़… इंसाफ़” सिस्टम के मुंह पर तमाचा हैं। यह उस टूटे हुए भरोसे का बयान है जो उसकी मौत की असली वजह है।
अब बात करें सियासी और सामाजिक असर की। इस केस ने मुज़फ़्फ़रनगर और आस-पास के ज़िलों में भारी रोष पैदा किया। धरना, विरोध, कैंडल मार्च—सब कुछ दिखा। लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि 7,000 रुपये की फीस विवाद से किसी की जान कैसे जा सकती है। यह रोष दरअसल उस सामूहिक असुरक्षा का इज़हार है जो हर गरीब छात्र महसूस करता है—कि कोई उसे सुनेगा या नहीं।
कांग्रेस पार्टी ने न्यायिक जांच की मांग की है। यह मांग वाजिब है, क्योंकि पुलिस खुद इस केस में आरोपी है। अगर स्थानीय पुलिस ही जांच करेगी, तो हितों का टकराव होगा। इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए judicial या magistrate inquiry बेहद ज़रूरी है।
सामाजिक रूप से देखें, तो यह घटना एक गहरी बीमारी की तरफ़ इशारा करती है—जहाँ शिक्षा का कारोबार बढ़ रहा है, मगर इंसानियत घट रही है।
आखिर में, मैं एक बड़ा सवाल छोड़ता हूँ: क्या यह घटना बदलाएगी?
अगर जांच निष्पक्ष हुई, अगर दोषियों को सज़ा मिली, अगर संस्थागत प्रणाली बदली—तभी इस मौत का कोई मायने होगा। वरना उज्ज्वल राणा सिर्फ़ एक और नाम बन जाएगा उन सूची में जो गरीब थे, मेहनती थे, और सिस्टम ने उन्हें कुचल दिया।