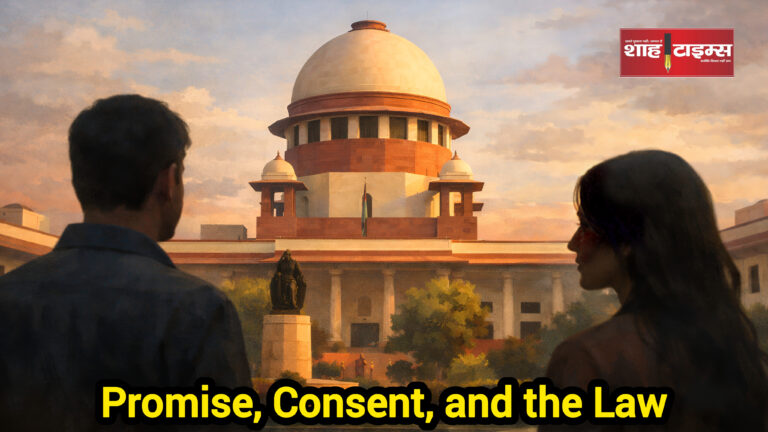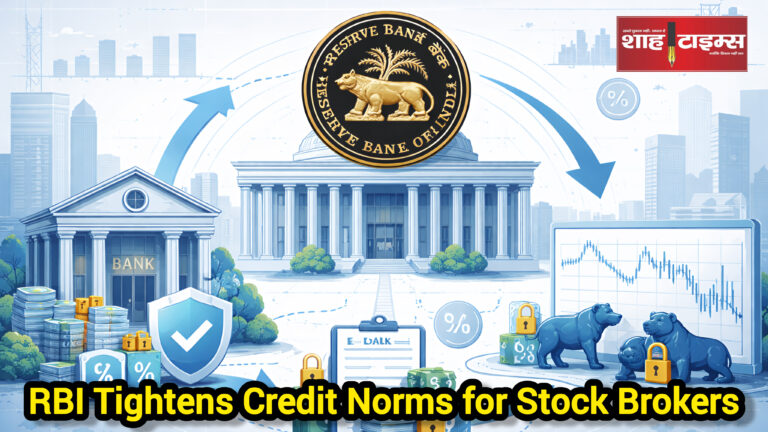Delhi smog and air pollution scene with low visibility and masked citizens
जब हवा ज़हर बनी: दिल्ली-एनसीआर का धुआँ और भारत की ज़िम्मेदारी
दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर ज़हर बन चुकी है। AQI 400 पार, GRAP-3 लागू, और बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सब सांस लेने को मजबूर हैं। सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं, पूरे मुल्क के जलवायु भविष्य का है।
📍नई दिल्ली 🗓️ 12 नवम्बर 2025 ✍️आसिफ़ ख़ान
दिल्ली की सर्द हवाओं में अब सिर्फ ठंड नहीं, एक ख़ामोश खौफ़ भी घुल चुका है। धुंध की परतें शहर को निगल रही हैं, जैसे आसमान खुद अब साँस लेने से इनकार कर रहा हो। बुधवार को दिल्ली का औसत AQI 413 पर पहुँचा, जबकि नोएडा 425 और गुरुग्राम 365 के पार गया। स्कूल बंद, निर्माण कार्य रुके, और लोग मास्क के पीछे छिपे — मगर सवाल वही है: आख़िर ये हालात बार-बार क्यों दोहराए जाते हैं?
GRAP-3 लागू है, पर राहत दूर है। पाँचवीं क्लास तक स्कूलों की छुट्टी, वर्क फ्रॉम होम की सलाह, और डीज़ल गाड़ियों पर पाबंदी — ये सब तात्कालिक उपाय हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं। हर साल नवंबर आते ही दिल्ली गैस चैंबर में बदल जाती है। और हर बार सरकारें वही बयान देती हैं — “स्थिति पर नज़र है।”
असलियत यह है कि समस्या सिस्टम से गहरी है।
यह सिर्फ “एयर पॉल्यूशन” नहीं, बल्कि हमारे विकास मॉडल की ग़लती है। खेतों में पराली जलाने से लेकर निर्माण स्थलों की धूल, पुराने वाहनों का धुआँ और कारख़ानों का उत्सर्जन — सब मिलकर इस शहर की रगों में जहर भर रहे हैं। मगर यह कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं, बल्कि लखनऊ से लेकर पटना और मुंबई तक एक जैसी है।
दिल्ली-एनसीआर: एक चेतावनी नहीं, एक मिसाल
दिल्ली आज जो झेल रही है, वो कल दूसरे शहरों की हक़ीक़त होगी। दिल्ली का प्रदूषण किसी एक शहर का अपराध नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत की सामूहिक नाकामी है। पंजाब-हरियाणा की पराली, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक इकाइयाँ, और दिल्ली की ट्रैफिक जाम मिलकर उस हवा को जहरीला बना रहे हैं, जिसे हम सब साँस के साथ भीतर खींच रहे हैं।
वक़्त आ गया है कि इस समस्या को “सीज़नल न्यूज़” की जगह “क्लाइमेट क्राइसिस” समझा जाए।
अगर धुंध में दबे सूरज को देखकर भी हम नहीं जागे, तो आने वाले बरसों में सिर्फ AQI नहीं, इंसानी उम्मीदें भी मुरझा जाएँगी।
भारत की क्लाइमेट हक़ीक़त
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है। और यही विरोधाभास है कि हम एक तरफ़ विकास की दौड़ में हैं, और दूसरी तरफ़ अपनी ज़मीन, हवा और पानी खो रहे हैं।
सरकारें COP समिट्स में “नेट ज़ीरो” की बातें करती हैं, मगर ज़मीनी सच्चाई यह है कि दिल्ली के लोग 24 घंटे में 20 सिगरेट के बराबर धुआँ अपने फेफड़ों में भर रहे हैं।
उर्दू की एक लाइन याद आती है —
“हवा में ज़हर घुला है, मगर इल्म का सन्नाटा है।”
यानि हम जानते हैं कि मर्ज़ क्या है, लेकिन इलाज पर अमल नहीं करते।
क्या है समाधान का रास्ता?
पहला कदम है — ज़िम्मेदारी का बँटवारा।
सिर्फ सरकार पर नहीं, बल्कि नागरिकों पर भी। अगर घरों में कोयला या लकड़ी जलाना बंद हो, अगर छोटी दूरी पैदल या साइकिल से तय हो, अगर हर मोहल्ले में पेड़ लगाने की परंपरा फिर शुरू हो — तो तस्वीर बदल सकती है।
दूसरा कदम — क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन।
भारत को सौर, पवन और हरित ऊर्जा की ओर तेज़ी से बढ़ना होगा। थर्मल पावर प्लांट्स की निर्भरता कम करनी होगी। दिल्ली की बसों को इलेक्ट्रिक में बदला जा रहा है, मगर स्केल और निगरानी अभी भी कमज़ोर है।
तीसरा कदम — शिक्षा और चेतना।
स्कूलों में बच्चों को क्लाइमेट साक्षरता सिखाई जाए।
जागरूकता सिर्फ “नो पॉल्यूशन डे” तक सीमित न रहे, बल्कि रोज़मर्रा का हिस्सा बने।
सरकार, उद्योग और नागरिक: तीनों की परीक्षा
सरकार अगर सख़्त कानून लाती है लेकिन उनका पालन नहीं होता, तो नीति व्यर्थ है।
उद्योग अगर CSR में “ग्रीन वॉशिंग” करते हैं, तो वो भी अपराधी हैं।
और नागरिक अगर सुविधा के लिए नियम तोड़ते हैं, तो यह आत्मघात है।
सच्ची तस्वीर यह है कि दिल्ली की हवा अब राजनीति से ज़्यादा, नैतिकता का इम्तिहान बन चुकी है।
“साँस लेना अब हक़ नहीं, लक्ज़री बन गया है।”
Science vs Silence
World Health Organization के मुताबिक, भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 7 उत्तर भारत के हैं। हर साल करीब 12 लाख लोग प्रदूषण से संबंधित बीमारियों से मरते हैं।
मगर हम अब भी आंकड़ों पर नहीं, मौसम पर बात करते हैं।
हम कह देते हैं, “ठंड आ रही है, धुंध बढ़ गई।”
असल में बढ़ा है तो सिर्फ हमारा सामूहिक मौन।
उम्मीद की किरण
हालात बदतर हैं, पर निराशा नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में कई नागरिक समूह जैसे Clean Air Collective और Warrior Moms ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। बच्चे मास्क पहनकर स्कूल जा रहे हैं, मगर साथ ही अपने स्कूल में पेड़ लगा रहे हैं। यही नई पीढ़ी शायद उस हवा को साफ़ करेगी जिसे हमने गंदा किया।
“जो हवा में ज़हर घोले, उसे भी एक दिन साँस लेनी है।”
यानी इंसान अगर प्रकृति से दुश्मनी करेगा, तो अंततः खुद उसका शिकार बनेगा।
Bottom Line
दिल्ली की हवा सिर्फ दिल्ली वालों की ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे भारत की चेतावनी है।
GRAP-3 हो या COP-29, असली लड़ाई ज़मीन पर है — जहाँ हर नागरिक को खुद को बदलना होगा।
साफ़ हवा कोई सुविधा नहीं, बल्कि अस्तित्व का सवाल है।